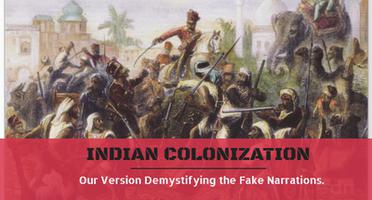महानंदा नदी अपडेट - बाढ़ नियंत्रण का तकनीकी पहलू
- By
- Dr Dinesh kumar Mishra
- September-28-2018
पृष्ठ भूमि
आम तौर पर यह माना जाता है कि जब किसी इलाके में बारिश इतनी ज्यादा हो जाय कि वहाँ के तालाब, पोखरे, नदी-नाले भर कर छलकने लगे और छलकता हुआ पानी ऐसी जगहों तक पहुँच कर टिक जाये जहाँ से उसकी निकासी आसान न हो तो कहा जा सकता है कि बाढ़ आ गई है। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी इलाके में बाढ़ आने के लिये उसी इलाके में बारिश हो । ऊपरी इलाकों में अच्छी बारिश होने पर निचले इलाकों में बिना पानी बरसे भी बाढ़ आ सकती है।
नदियों में उनकी समाई से ज्यादा पानी आ जाने की वजह से उनका
छलकना और आस-पास के इलाकों को डुबाना, नदियों
और उनकी सहायक नदियों में एक साथ पानी का चढ़ना और कभी-कभी मुख्य नदी के पानी का
उल्टा सहायक धारा में बहना, किसी
खास इलाके में जबर्दस्त बारिश, चट्टानें
खिसकने या बर्फ की शिलायें खिसकने की वजह से नदियों के बहाव में रुकावट और नदी के
पानी का इन रुकावटों के ऊपर होकर या तोड़ कर बहना, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ऊँचे-ऊँचे ज्वार का
उठना और इसके साथ ही नदियों में उफान, तूफान
और चक्रवात, और इसके अलावा पानी की
निकासी न हो पाने की वजह से भी बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। तकनीकी भाषा में
ऐसा कहा जाता है कि जब तेज बारिश या नदी नालों के छलकते पानी या पानी की निकासी
में दिक्कतों की वज़ह से रोज़ मर्रा की ज़िन्दगी पर खतरा पड़ने लगे तो मानना
चाहिये कि बाढ़ आ गई है। वक्त के साथ बाढ़ और उससे होने वाली तबाहियों के रिकॉर्ड
कायम हुआ करते हैं। किसी भी बाढ़ के बारे में यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि
यही सबसे खतरनाक बाढ़ है। तबाहियों और बरबादियों के रिकॉर्ड भी टूटने के लिये ही
बनते हैं।
यह मुमकिन है कि शुरू-शुरू में बाढ़ से बचाव की कोशिशें
व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर की रही हों और लोगों ने अपने जान माल की हिफाज़त के
लिये अपनी लड़ाई खुद लड़ी हो पर जैसा कि बाढ़ समस्या का स्वरूप होता है उसके
मुताबिक इसके सामाजिक और राज्य सत्ता स्तर तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगी
होगी। इन कोशिशों में बाढ़ से बचाव के नये-नये तरीके ईजाद हुये और आज इस समस्या से
निबटने के लिये जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध है उसको थोड़ा समझने की कोशिश हम यहाँ
करेंगे। यह सारे उपाय तकनीकी समाधान की श्रेणी में आते हैं। प्रचलित भाषा में इसे
संरचनात्मक समाधान (Structural Solution) कहते हैं।
बड़े बाँध
बाढ़ से निबटने का एक आधुनिक तरीका बड़े बाँध बना कर पानी की रफ्तार और आमद पर वहीं काबू कर डालने का है जहाँ नदी पहाड़ों से नीचे उतरने को होती है। ऐसे बड़े बाँध बना कर उनके नीचे उतना ही पानी छोड़ने का इन्तजाम किया जाता है जिससे कि मैदानी इलाकों में बाढ़ न आये। आम तौर पर ऐसे बाँध कंक्रीट या पत्थर से बनाये जाते हैं। कभी-कभी नदी को पहाड़ों से मैदान में उतरने के बाद मिट्टी के बाँधों से बाँध दिया जाता है और इसमें गैर जरूरी पानी की निकासी के लिये पत्थर या कंक्रीट के स्पिल-वे की व्यवस्था कर दी जाती है। इस तरह के बाँधों में अमूमन सिंचाई करने तथा बिजली पैदा करने का भी इन्तजाम रहता है। इसके अलावा मछली पालन, मनोरंजन, नौ-परिवहन वगैरह बहुत से फ़ायदे भी इस प्रकार के बाँधों से उठाये जा सकते हैं। इस वज़ह से ऐसे बाँधों को बहुद्देशीय बाँध (Multi purpose Dam) भी कहते हैं।
इस तरह के बाँधों का प्रचलन बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दौर
में देखने में आया जबकि यह बाँध आधुनिक विज्ञान और तकनीक का शाहकार समझे जाते थे।
इन बाँधों की मदद से सारी दुनियाँ में सिंचाई, बिजली, बाढ़
नियंत्रण आदि समस्याओं के समाधान के सपने देखे गये। खुद हमारे देश में भाखड़ा, हीराकुड, नागार्जुन सागर, मेटूर, मयूराक्षी, तिलैया, पांचेत, मैथन, तुंगभद्रा आदि कितने ही
बाँध अज़ादी के बाद बने और एक लम्बी सूची ऐसे बाँधों की है जिन पर या तो काम चल
रहा है या उन पर भविष्य में हाथ लगने की उम्मीद है। ‘आधुनिक भारत के मन्दिर' की उपाधि से विभूषित इन
बाँधों से होने वाले फायदों से जितनी उम्मीदें लोगों ने लगाई थीं उतना हासिल नहीं
हो सका जिसकी वजह से न सिर्फ इनकी चमक फ़ीकी पड़ी है बल्कि इन बड़े बाँधों की
उपयोगिता पर भी उंगलियाँ उठने लगी हैं। आज से क़रीब पचास साल पहले इन बड़े बाँधों
का जादू नेताओं और इन्जीनियरों और यहाँ तक कि आम जनता के सिर पर चढ़ कर बोलता था
क्योंकि इनकी बुनियाद पर सभी ने कुछ न कुछ सपने बुने थे। आज हालात बदल गये हैं
क्योंकि इन पचास वर्षों के अन्दर लोगों के तजुर्ब बढ़े हैं और बड़े बाँधों के सवाल
पर बाँधों के समर्थकों और विरोधियों ने अपने-अपने खेमें अलग-अलग गाड़ लिये हैं।
जरूरत इस बात की है कि इनकी दलीलों पर एक नज़र डाली जाय और तब कोई राय बनाई जाय।
जैसा कि हम पहले कह आये हैं बड़े बाँधों से मोटे तौर पर
नहरों से सिंचाई कर के लहलहाते खेत, जल
विद्युत केन्द्रों से पैदा हुई बिजली से जगमगाती बस्तियाँ और हमेशा समृद्धि की ओर
कदम बढ़ाते हुये उद्योग, बाढ़
से साल दर साल होने वाली तबाहियों का जड़ से खात्मा, जैसी बातें खास तौर पर कही जाती हैं। आश्वस्त खेती, बढ़ती हुई रोज़गार की
सम्भावनायें, चारो तरफ फैलती खुशहाली
और इनके साथ ही आधुनिकतम तकनीक से बनने वाले विशालकाय बाँधों का अपने देश या
क्षेत्र में होने का गौरव किस को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अमेरिका की टेनेसी
वैली अथॉरिटी (TVA) ने टेनेसी नदी घाटी में
अनेक ऐसे बाँध बनाये थे जिनकी तर्ज पर हमारे देश में पाँचवें दशक में दामोदार घाटी
निगम (DVC) की स्थापना हुई। स्वयं
भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू टेनेसी घाटी के बाँध देखने
गये थे। 28 अक्टूबर 1949 को जब वे अमेरिका में
नॉक्सविले में मॉरिस बाँध देखने गये तो उन्हें लगा कि उनके जीवन का एक सपना साकार
हो गया। इस बाँध की ऊँचाई महज़ 72.6 मीटर थी। उसके बाद खुशहाली और बेहतर जिन्दगी की तलाश में 1979 आते-आते भारत में 1554 ऐसे बाँधों की बुनियाद
रखी जा चुकी थी और यह कोशिशें आज भी जारी हैं।
जब देश को आज़ादी मिली थी उस समय अन्न के मसले पर हम आत्म
निर्भर नहीं थे जबकि आज हमें अनाज का आयात नहीं करना पड़ता है। इसी तरह आजादी के
समय देश में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1360 मेगावाट थी जो कि 1981-82तक बढ़कर 32,345 मेगावाट हो गई। यह कोई मामूली बात नहीं है कि यह क्षमता
नब्बे के दशक के शुरू में 64,000 मेगावाट तक पहुँच गयी। बिजली की यह माँग समय के साथ बढ़ती
ही जायगी और एक अनुमान के अनुसार इस सदी के आखिर तक अपनी जरूरतें पूरी करने के
लिये हमें 1.08 लाख मेगावाट बिजली का
उत्पादन करना होगा। फिर, इस सदी
के अन्त तक हमारे देश की आबादी भी 100 करोड़ को छूने लगेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिये अनाज का
उत्पादन भी हमें करना होगा। बड़े बाँध बना कर जलाशय के नियंत्रण से निचले इलाकों
में बाढ़ों से साल दर साल होने वाले नुकसान को रोका भी जा सकेगा।
इन दलीलों से इत्तिफ़ाक रखने वाले लोग यह मानते हैं कि
हमारी समस्याओं का समाधान बड़े बाँधों में निहित है और इनका विरोध करना एक
अराष्ट्रीय काम है।
एन० सी० मेनन (1992) का कहना है, “...1979 में फ्यूज़न एनेर्जी
फाउन्डेशन द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि भारत के आर्थिक विकास की
कुंजी वहाँ के वृहद जल स्रोतों के सही उपयोग में है जिससे कि आधुनिक कृषि के
रास्ते में आये सूखे और बाढ़ जैसे अवरोधों को हटाया जा सके।“
(अध्ययन में) एक तीस वर्षीय योजना का प्रस्ताव है जिसके तहत
बाँध, जलाशय, नहर प्रणाली, न्यूक्लियर औद्योगिक
केन्द्र, जिन्हें प्रचलित भाषा में
न्यूप्लेक्स कहते हैं, बनाने
का प्रस्ताव है जिसमें कृषि उद्योगों और आणविक ऊर्जा का सामंजस्य होगा। ...परन्तु
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भारत द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से तकलीफ़ होती
है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विकसित, औद्योगिक और सम्पन्न देश भारत और चीन के विरुद्ध आणविक
अनुसंधान, मिसाइल और अंतरिक्ष जैसे
पहलुओं पर मोर्चा साध लेते हैं। जिन्होंने खुशहाली और सम्पन्नता तक की मंज़िलें तय
कर ली हैं वह कभी नहीं चाहते कि दूसरे वहाँ तक पहुँचे और अगर यह गोरे लोग नहीं हैं
तब तो एक दम नहीं।
...जाहिर है कि जो लोग
नर्मदा परियोजना का विरोध कर रहे हैं उनके लिये विरोध का वैज्ञानिक या तकनीकी कारण
खोज पाना तो नामुमकिन है तो उन्होंने मानवाधिकार जैसे भावनात्मक पहलुओं का आश्रय
लिया।.. यह उत्साही, उपद्रवी
लोग नर्मदा जैसी परियोजनाओं के लिये समस्या बने रहेंगे और इनका कोई तैयार या सुलभ
समाधान भी नहीं है। संबद्ध सरकारों को यह चाहिये कि लोगों को समझा बुझा कर और पूरी
जानकारी देकर साथ लेकर चलने की कोशिश करें। इस सन्दर्भ में यह जरूरी हो जाता है कि
अनाज और बिजली पैदा करने के जो भी जरिये हाथ लगें उनका इस्तेमाल किया जाय। बड़े
बाँधों का निर्माण इसी तरह का एक जरिया है। यह एक ऐसा मसला और ऐसी मजबूरी है जिस
पर किसी तरह की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा बड़े बाँधों के समर्थकों का मानना है। ज़ाहिर तौर पर यह
दावे एक दम दुरुस्त लगते हैं।
अब एक नज़र उन दलीलों पर भी दौड़ायें जो कि इन दावों से मेल नहीं खाती।
बड़े बाँधों के साथ पहली परेशानी भूकम्प को लेकर आती है।
गंगा घाटी का निर्माण तो ज़मीन के दो टुकड़ों के मिलाप से हुआ है। गोण्डवाना लैण्ड
वाला हिस्सा क़रीबन 5 से०
मी० प्रति वर्ष के हिसाब से उत्तर की ओर खिसकता है जिससे एशियाई ज़मीन पर दबाव बना
रहता है। कभी-कभी यह प्लेटें सरक जाती हैं जिसकी वजह से पूरे हिमालय क्षेत्र में
खतरनाक भूकम्प आते रहते हैं। पिछले सौ वर्षों में हिमालय के इलाके में 1897 (असम), 1905 (काँगड़ा), 1918 (श्री मंगल-असम), 1920 (दिल्ली), 1930 (धुबरी-असम), 1934 (बिहार-नेपाल), 1950 (असम), 1975 (कन्नौर-लाहौल स्पिती), 1988 (बिहार), 1991 (उत्तर काशी) में काफ़ी
बड़े भूकम्प आये हैं जिनसे जान-माल की भारी तबाहियाँ हुई हैं। दुर्भाग्य वश गंगा
घाटी में बनने वाले सारे बाँध इन्हीं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में बनेंगे जिनसे
इनकी सुरक्षा पर हमेशा सवालिया निशान लगे रहेंगे।
इन बाँधों की डिजाइन में वैसे तो भूकम्प के झटकों को
बर्दाश्त करने का प्रावधान किया जाता है जिससे कि भूचाल आने की स्थिति में कोई
हादिसा न हो। अमूमन इंजीनियर इस बात पर इत्मीनान कर लेते हैं कि बाँध की डिजाइन
में भूकम्प बर्दाश्त कर लेने का इन्तजाम कर लिया गया है। बड़ा बाँध बनने की वजह से
ज़मीन पर जो पानी, कंक्रीट
वगैरह का अतिरिक्त वज़न पड़ता है, उसकी
वज़ह से भी ज़मीन के नीचे की प्लेटों में हरकत आती है और इसके कारण भी भूकम्प के
झटके आते हैं। मगर क्योंकि बाँधों की डिज़ाइन में भूकम्प बर्दाश्त करने का प्रावधान
रहता है इसलिये इंजीनियर लोग बाँध बनाने की वज़ह से आने वाले भूकम्पों को खास
तरजीह नहीं देते।
फिर भी यह सच है कि 1897 और 1950 में असम में आये भूकम्पों से भारी तबाही हुई थी। झटका तो
असम में 1988 (अगस्त) में भी कम नहीं
लगा था पर बरबादी टल गई थी। 1934 के उत्तर बिहार में आये भूकम्प की दास्तान कहने वाले लोग
अभी भी जिन्दा हैं और 1988 वाले भूकम्प से नेपाल के धरान और भारत के मधुबनी और दरभंगा
जिलों में जो तबाही हुई उसकी भरपायी अभी तक नहीं हुई है। अक्टूबर 1991 के उत्तर काशी के भूकम्प
ने टिहरी में बन रहे पहले से ही विवादास्पद बाँध के निर्माण के विरोध में श्री
सुन्दरलाल बहुगुणा को फरवरी 1992 में आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। जैसे तैसे अप्रैल 1992 में यह अनशन टूटा जबकि
प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि पूरी योजना का पुनर्मूल्याङ्कन किया जायगा।
आजकल बाँधों के रूपाङ्कन के साथ-साथ यह जरूरी माना जाने लगा
है कि बाँध टूटने की स्थिति में इस दुर्घटना से होने वाले नुकसान का अंदाजा पहले
से लगा लिया जाय। यह इसलिये भी जरूरी है कि अगर कभी दुर्भाग्य से ऐसी दुर्घटना हो
गई तब बचाव और राहत कार्य की पूरी तैयारी पहले से रहेगी। परन्तु बाँध निर्माण के
इस पक्ष पर परदा डालने की कोशिशें चलती रहती हैं। टिहरी बाँध के सन्दर्भ में प्रो०
टी० शिवा जी राव (1992) कहते
हैं कि “टिहरी बाँध के टूटने की
परिस्थिति में जनता के स्वास्थ्य और कल्याण में उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय
ऊर्जा मंत्रालय की कोई रुचि नहीं दिखती है और इसलिये ये पर्यावरण के व्यापक
सन्दर्भ में परियोजना के सुरक्षात्मक पहलुओं का निर्धारण करने वाले आपदा प्रबन्धन
योजना (Disaster Management Plan) को
पर्यावरण मंत्रालय भेजने से आनाकानी कर रहे हैं।.... प्रारम्भिक अनुमानों के
अनुसार अगर किसी भी वजह से वह बाँध टूटता है तो पूरा जलाशय आधे घन्टे में खाली हो
जायगा और अचानक आई बाढ़ में देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरद्वार समेत गंगा घाटी
के बहुत से गाँवों और कस्बों का सफ़ाया हो जायगा। आँखें बन्द कर के योजना का
समर्थन करने वाले परामर्शियों और विशेषज्ञों को, जो कि परियोजना के पर्यावरण पर होने वाले असर पर किसी भी
सार्वजनिक बहस को एकदम खारिज कर देते हैं, यह चाहिये कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माँगी गई डिसास्टर
मैनेजमेन्ट रिपोर्ट जमा कर के अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित करें। यदि परामर्शी विशेषज्ञ
उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के उन लोगों के साथ, जिनका बाँध टूटने की
परिस्थिति में बचाव या पुनर्वास करना पड़ेगा, मिल बात करके डिसास्टर मैनेजमेन्ट प्लान बनाने से डरते हैं
जिससे करोड़ो लोगों के जीवन, कृषि, यातायात, स्मारकों एवम् पवित्र
मंदिरों पर आने वाले खतरे की हकीकत सामने आयेगी तब वे कैसे उन लोगों में दोष
निकालते हैं जो कि लोकसभा के अन्दर और बाहर एक सार्वजनिक बहस की माँग कर रहे हैं।
जिससे कि इस विवादास्पद परियोजना से होने वाले नफ़े और नुकसान का खुलासा हो सके।
भूकम्पों के कारण बाँधों का टूटना महज़ दिमागी फ़ितूर नहीं
है। यह एक ज़िन्दा हक़ीक़त है। ‘दुनियाँ
के 8,925 बाँधों में से अब तक 535 बाँधों के टूटने की
पुष्टि हुई है जिसमें 202 मामलों में घटना ने विभीषिका का रूप धारण कर लिया। भारत के 433 बड़े बाँधों में से बाँध
टूटने की 40 वारदातें (1874 से 1975 के बीच) हुई हैं जिसमें
से 13 हादिसे खतरनाक थे । हिमालय
के इलाके में बनने वाले बाँध निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर एक नंगी तलवार
की शक्ल में हमेशा झूलते रहेंगें। हमारे यहाँ 1962 में महाराष्ट्र में खड़गवासला तथा पान्शेत बाँधों के टूटने
की वारदातें हो चुकी हैं जिससे जानमाल की व्यापक क्षति हुई थी। महाराष्ट्र में ही 1967 में कोयना बाँध में दरार
पड़ने से कोयना शहर और आसपास के इलाकों में जबर्दस्त तबाही हुई थी। 1971 में गुजरात का मोरवी शहर
माचू बाँध के टूटने की वज़ह से बरबाद हुआ था।
बात सिर्फ़ भूकम्प के बड़े झटकों तक ही सीमित नहीं है, छोटे-मोटे झटके भी अपने
तरीके का सदमा पहुँचाते हैं। ऐसे झटकों से पहाड़ों की ज़मीन खिसकती है और टूटते
कगारों की मिट्टी नदी में गिर कर पानी की रफ्तार को रोक तक देती है। 1880 में उत्तर प्रदेश में
पहाड़ों में जमीन खिसकने के कारण नैनीताल के आस पास की पहाड़ियाँ बह गई थीं और
नैनीताल झील का खात्मा हो गया था। सितम्बर 1893 में बिरही नदी में दो बड़ी चट्टानें गिर जाने से नदी का
पानी पहले तो ठहर गया फिर 1894 में किनारे तोड़कर बह निकला और अपने पीछे गंगा घाटी के ऊपरी
इलाकों में तबाही के निशान छोड़ गया। इधर हाल में 1970 में जोशीमठ के पास जमीन खिसकने से एक बार फिर पानी रुका और 1894 की दास्तान दुहराई गई।
उसी जगह 1978 में वैसा ही हादिसा फिर
पेश आया।
बड़े बाँध बनने से हलके फुलके भूकम्पों की तादाद में
बढ़ोतरी होगी, ऐसा सभी मानते हैं। ऐसा न
भी हो तब भी ज़मीन खिसकने की वज़ह से नदी में आया सारा मलवा बाँध के जलाशय में
इकट्ठा होगा और इससे बाँध का जीवन काल कम होगा। वैसे भी नदी के पानी के साथ आने
वाली मिट्टी/ रेत जमते-जमते बाँध के पीछे के जलाशय की जिन्दगी को रोज़-ब-रोज़ घटाती
है। जलाशय में जमा होने वाली मिट्टी/रेत का पहले से किया गया अन्दाज़ा अक्सर ग़लत
होता है। जलाशय में जमा होने वाली मिट्टी / रेत की दर पूर्वानुमानित दर के मुकाबले
निज़ाम सागर बाँध में 16 गुने, मसानजोर में तीन गुने, मैथन में 8 गुने, पांचेत हिल में 4 गुने से ज्यादा तथा
भाखड़ा में डेढ़ गुनै के आस पास है। टिहरी बाँध में यह दर अनुमान से 1.65 गुने से भी अधिक है। इस
तरह से बाँध की जिन्दगी में घुन लग जाता है। इसी तरह की एक और परेशानी भुरभुरे
मिट्टी के ढेर की शक्ल में स्थित पहाड़ों के क्षेत्र में सड़क निर्माण के कारण भी
है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद
सड़क निर्माण की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। इन सड़कों के निर्माण के लिये काफी
मिट्टी इधर से उधर करनी पड़ती है जिसका अधिकांश नीचे नदी घाटी में पहुँच जाता है।
हिमालय के क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई प्रायः 44,000
कि० मी० है और इतनी लम्बी सड़क के निर्माण में 17600 से 35200 लाख घन मीटर मिट्टी की
क्षति होती है। सड़कों के रख रखाव में प्रति कि० मी० 550 घन मीटर मलवा हर साल निकलता है। यह सारी मिट्टी नदियों के
माध्यम से जलाशयों में पहुँच जायगी और उनके जीवन काल को घटायेगी और सड़कों का
निर्माण एक न रुकने वाली प्रक्रिया है।
बाँधों पर युद्ध के दौरान हमले की वारदातों की नज़ीर मिलती
है। जब दुश्मन को नुकसान पहुँचाना ही अकेला फर्ज बचा रहता है तब बाँधों तक को
निशाना बनाया जाता है। उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के आपसी झगड़े में बाँधों पर हमले
हुये हैं। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ी फौज़ों ने जर्मनी में बने बाँधों की
बखिया उधेड़ी है। मोजाम्बीक की घरेलू लड़ाई में यह बाँध मोहरे बने हैं और
एल-सल्वाडोर में भी इन बाँधों को नज़र लग गई है। यह सारा मुद्दा इसलिये और अहम हो
जाता है कि एक अच्छे खासे इलाके की सिंचाई, बिजली का उत्पादन, और
बाढ़ नियंत्रण एक ही संरचना पर केन्द्रित होता है और यह बाँध अपने आप हमलावरों की
नज़रों में चढ़ते हैं। भारतनेपाल के पारस्परिक सहयोग से नेपाल में कई बड़े बाँधों
के निर्माण की बात चीत एक लम्बे अरसे से चल रही है। इन बड़े बाँधों की सामरिक
सुरक्षा हमारे लिये बहुत ही विचारणीय विषय है। बड़े बाँधों के साथ एक परेशानी उनके
लागत खर्च और उनके निर्माण में लगने वाले समय की भी है। बिहार के फ़ायदे के लिये
नेपाल में कोसी नदी पर प्रस्तावित बहूद्देशीय बाराह क्षेत्र बाँध का ही एक उदाहरण
लें। इस बाँध की कुल लागत 1947 में 100 करोड़ रुपये, 1952 में 177 करोड़ रुपये, 1981 में 4054 करोड़ रुपये थी और फिलहाल इसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये के आस पास
बताई जाती है और यह सब ज़बानी जमा खर्च है, क्योंकि यह बाँध अभी तक चर्चा की हदों
से बाहर नहीं आया है। अगर इस बाँध के काम पर आज ही हाथ लगे तो इसको बनते-बनते लगभग
30 साल और गुज़र जायेंगे और
तब तक इसकी लागत कहाँ पहुँचेगी और इतनी बड़ी रकम कहाँ से आयेगी। यह शक बेबुनियाद
नहीं है क्योंकि उत्तर बिहार में बनने वाली कोसी परियोजना की अनुमानित लागत 1953 में 37.31 करोड़ रुपये थी और 1985 में आधी अधूरी इस योजना
के फ़ेज़I की समाप्ति तक 180 करोड़ रुपये खर्च हुये
थे। इस योजना के फ़ेज़ में 123.85 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी तरह 1959 में गण्डक परियोजना की
अनुमानित लागत 40:43 करोड़ रुपये थी और 1985 में फ़ेज I की समाप्ति तक इस योजना
पर क़रीब 366 करोड़ रुपये खुर्च हुये और
फ़ेज़ में 445.23 करोड़ रुपयों की माँग की
गई है ख़र्च की रफ्तार अगर यही मान ली जाय तो 12,000
करोड़ रुपयों वाली योजना का क्या हाल होगा? अगर कोसी और गण्डक
परियोजनाओं की तरह इस बाँध की लागत भी दस से पन्द्रह गुना बढ़ी, और आश्चर्य तभी होगा अगर
ऐसा न हो, तो योजना के पूरा होते न
होते लगभग 1,50,000 करोड़ रुपयों की आहुति दे
देनी पड़ेगी। 1993 में हमारे देश पर लगभग 2,70,000 करोड़ रुपयों का विदेशी
कर्ज था। यह बाँध भी क़र्ज़ लेकर ही बनेगा। इस तरह की 16 योजनायें नेपाल की पहाड़ियों में विचाराधीन हैं। और अगर सब
पर काम शुरू हो तो पैसा सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, या फिर अन्य विदेशी
संस्थाओं से कर्ज की शक्ल में ही आयेगा। इतना क़र्ज़ लेकर हम किस-किस गली से
गुज़रना छोड़ देंगे।
इसके बावजूद हमारे देश पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिये
बाहरी संस्थायें हमें आसानी से कर्ज दे देगीं क्योंकि समय पर ब्याज चुकाने की
हमारी साख कायम है और मूलधन में कब किसी महाजन की दिलचस्पी रही है। उसके बदले में, ब्याज के अलावा, हम उन्हें परामर्शी
सेवाओं के लिये मोटी रकम वापस करेंगे, उनकी
घटिया और बेकार पड़ी मशीनें आयात करेंगे, उनके
बेरोजगारों को अपने यहाँ विशेषज्ञ बना कर सिर आँखों पर रखेंगे और उन्हीं की
कम्पनियों को ठेके देंगे। इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर क्या यह नहीं होगा
कि अपनी क्षमता और ताकत के अनुरूप हम अपनी योजनायें खुद बनायें। दर असल विकास की
चकाचौंध दिखाकर कर्ज देने की पेशकश के पीछे विकसित देशों के अपने निहित स्वार्थ
हैं। इस तरह के कर्जे न सिर्फ बाहरी संस्थाओं पर हमारी निर्भरता को बढ़ाते हैं
बल्कि देश की गरीबी को भी बेतहाशा बढ़ाते हैं। ऐसा इस लिये होता है कि शुरू शुरू
में तो आसानी से मिल जाने वाले इस कर्ज़ से बड़ी सुविधा मालूम होती है और इस तरह
अपने साधन जुटा पाने की कोशिश को ही नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है। राजनीतिज्ञ इस
तरह की विदेशी सहायता की बुनियाद पर उन योजनाओं का भी औचित्य सिद्ध करने की कोशिश
करते हैं जिनको किसी भी तरह वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में तीसरी दुनियाँ
के ज्यादातर देश इस तरह के कर्जी के शिकार हैं जिसमें उन देशों के नेताओं ने लोगों
को सब्जबाग दिखाने के बहाने और अपनी गद्दी पर आँच न आने देने के लिये अपने देश की
जनता को इन कर्जी के गड्ढे में ढकेला है। बड़े बाँधों के साथ जुड़ी हुई एक अहम
समस्या लोगों के विस्थापन और पुनर्वास की है। जहाँ बाढ़ आती है वहाँ के लोगों की
अपनी परेशानियाँ- होती
हैं यद्यपि बाढ़ के फ़ायदे कम नहीं हैं क्योंकि हर साल खेतों पर पड़ने वाली नई
मिट्टी से ज़मीन की उर्वराशक्ति तरोताज़ा हो जाती है। परन्तु निचले इलाकों में
बाढ़ को रोकने के लिये ऊपरी इलाकों में जहाँ बाँध्र बनते हैं वहाँ तो बाढ़ की कोई समस्या ही नहीं होती। बाँध बनने
पर वही इलाके डूबते हैं जिनका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं होता। बड़े बाँध बनने के
कारण एक अच्छी खासी आबादी निचले इलाकों की खुशहाली के लिये अपनी खुशियों और
तरतीबवार ज़िन्दगी की क़ुरबानी देती है जिसका एहसान कोई नहीं मानता। कहने को तो
पुनर्वास का मुआवजा तय होता है और लोगों को पहले से बेहतर स्थिति में पहुँचा दिया
जाता है पर अक्सर विस्थापित होने वाले लोगों को वादों की ही सौगात मिल पाती है।
ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के
बदले घर, सबको शिक्षा, परिवार के एक सदस्य को
परियोजना में नौकरी, स्कूल, सड़क, पानी की सुविधा, व्यवसाय शुरू करने के
लिये ट्रेनिङ्ग की व्यवस्था, आसान
शर्तों पर धन का जुगाड़, जैसे
कितने ही वादे हैं जो कि कर डाले जाते हैं। इनमें से कितने वादे पूरे होते हैं यह
अपने आप में शोध का विषय है। 7 जुलाई 1956 को पटना के एक अंग्रेज़ी
दैनिक दि इन्डियन नेशन में कोसी परियोजना के पुनर्वास पर एक लेख छपा था। उसका कुछ
हिस्सा इस प्रकार है--“योजना
शुरू होने के पहले से ही पता था कि इन गाँवों में बाढ़ से जिन लोगों के घर या
ज़मीन पर विनाश का खतरा आयेगा उन्हें घर के बदले घर तथा ज़मीन के बदले जमीन दी
जायगी । उन दिनों अधिकृत न होने पर भी कोई भी आदमी किसी भी तरह का भाषण दे दिया
करता था। वे लोग भी जो कि कुछ कहने के लिये अधिकृत भी थे वे भी उतने गंभीर नहीं थे
क्योंकि वे जानते थे कि आश्वासनों का कोई मतलब नहीं होता है। ...प्रारम्भिक दिनों
में इस मुद्दे को उभरने से रोका गया क्योंकि इससे योजना की लागत बढ़ जायगी और इससे
योजना के ही अस्वीकृत होने का अंदेशा था। इस योजना पर 1955 में काम शुरू हुआ था और इस बात का इन्तज़ार किया गया कि
वक्त के साथ लोग पुनर्वास की बात भूल जायेंगे मगर लोगों ने पुनर्वास की खानापूरी
पर कभी रजामन्दी की मुहर नहीं लगाई। 32 साल
बाद 30 जनवरी 1987 को सरकार ने कोशी पीड़ित
विकास प्राधिकार की स्थापना की ताकि लोगों के आर्थिक पुनर्वास पर काम किया जा सके।
यह एक अलग बात है कि यह प्राधिकार भी कुछ काम नहीं करता है।
कोसी योजना में तटबन्धों के बीच बसने वाले परिवारों की संख्या 1970 में 45,291 थी जिन में से 2,528 परिवारों के पक्के मकान थे। योजना में पुनर्वास की मद में 2,12,67,390/- रुपयों का प्रावधान था। 197273 तक मात्र 1,75,28,392/- रुपये खर्च हो पाये थे। कुल 32,540 परिवारों को घर बनाने के लिये अनुदान मिला जिसकी दूसरी किस्त सिर्फ 10,580 परिवारों को मिल पाई और एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसको घर बनाने की तीसरी और आखिरी किस्त मिली हो। शायद ऐसी वादा खिलाफ़ी का ही सीखा हुआ सबक था कि विश्व बैंक पोषित सुवर्णरेखा परियोजना में लगभग 12,800 परिवारों ने पुनर्वास की बात योजना लागू होने से पहले उठाई। पुनर्वास का जो मसला यहाँ मान-मनौवल से शुरू हुआ था वह थाना-पुलिस की यात्रा तय करता हुआ लाठी-गोली के मुकाम पर जा कर ठहरा जब कि 4 अप्रैल 1982 को गंगा राम कालुंडिया की शहादत हुई। इसी तरह टिहरी बाँध में 85,600 लोगों के पुनर्वास की फाँस अटकी हुई है।22 टिहरी बाँध की दिक्कतें तो पुनर्वास की हदों से आगे बढ़ चुकी है। यहाँ तो भूकम्प का प्रभाव, लागत खर्च, रूसी इंजीनियरों से डिजाइन पर मतभेद, स्थानीय लोगों का विरोध और अब सोवियत संघ के विघटन के बाद की कठिनाई आदि सारे मुद्दे उभर कर ऊपर आते है। वहाँ 27 फरवरी 1992 को श्री सुन्दरलाल बहुगुणा को अपने सहयोगियों के साथ धरना देते हुये गिरफ्तार किया गया जिन्हें 4 मार्च को छोड़ा गया । उधर नर्मदा परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना में लगभग 67,000 और इन्दिरा सागर परियोजना में लगभग 1.29 लाख लोगों के पुनर्वास को लेकर गतिरोध जारी है। यह गतिरोध विस्थापित होने वाले लोगों की वास्तविक संख्या से लेकर पुनर्वास के पूरे पैकेज में झलकता है। नर्मदा परियोजना के विरोध में नर्मदा बचाओ आन्दोलन' की सुश्री मेधा पाटकर ने जल समाधि लेने का प्रण किया था मगर सरकार द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन का आश्वासन देने पर यह अघटन टाला जा सका पुनर्वास का पूरा मसला वादों की उलझनों में अटका हुआ है। इस तरह के वादों में से एक वादे को वादा-ए-फ़र्दा, यानी कल पूरा किया जाने वाला वादा, कहते हैं जो कि न पूरा करने के लिये ही किया जाता है। कोसी वाले इलाके के लोग यह फरेब खा गये मगर आज के विस्थापित होने वाले लोग ज्यादा समझदार हैं। बकौल शायर,
‘हम ऐसे अहले तमाशा न थे जो होश आता हमें तुम्हारे तग़ाफुल ने होशियार किया।
बड़े बाँधों की मदद से बाढ़ रोकने की खुशफ़हमी आम लोगों के
दिमाग में काफ़ी गहरे पैठी हुई है। जब भी बाढ़े आती हैं तो नदी विशेष पर बाँध
बनाने का चर्चा तेज़ हो जाता है। बिहार के मामले में तो ऐसी नदियों की तादाद कुछ
ज्यादा ही है। यहाँ बाढ़ नियंत्रण की जय यात्रा दामोदर घाटी निगम के बाँधों से
दक्षिण बिहार में शुरू हुई थी। इस निगम की स्थापना 1943 में नदी घाटी में आयी अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई थी।
राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980), की रिपोर्ट के अनुसार, “लेकिन 1943 की बाढ़, जो
केवल १.911 क्यूमेक (3.5 लाख क्यूसेक) थी, तो प्रलय थी जिसके परिणाम
स्वरूप एंव किनारे का तटबन्ध टूट गया जिससे रेलवे लाइन और जी० टी० रोड कई स्थानों
पर टूट गई। मगर 1978 में
पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी निगम के बाँध बनने के बाद एक बार फिर जबर्दस्त बाढ़
आयी जिसमें दामोदर घाटी क्षेत्र के निचले इलाकों में निगम के बाँधों के बावजूद
बर्द्धमान, हुगली, हावड़ा, बाँकुड़ा और मेदिनीपुर
जिलों में बर्बादी की नयी दास्ताने लिखी गईं।
यह बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई थी और इस वक़्त सिंचाई और बिजली के उत्पादन को ध्यान में रखकर निगम के सारे जलाशयों को पूरा-पूरा भर कर रखा गया था। जब तेज़ बारिश शुरू हुई तो सारे कन्ट्रोल दरवाजे दहशत में खोल दिये गये। तब एक ओर बारिश के पानी और ऊपर से जलाशयों से छोड़े गये पानी की दोहरी मार लोगों पर पड़ी। मगर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट कहती है कि इस बात को फिर से याद | करना उपयोगी रहेगा कि 1943 की बाढ़ से जो तबाही हुई थी, उसी को देखते हुये दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर से आगे अब जितना अधिक औद्योगिक विकास हुआ है, उसे देखते हुये 1959 या 1978 की बाढ़ के कारण बायें किनारे में दरार आ जाने की सूरत में जो हानि होती उसकी कल्पना से भी डर लगता है। यदि दामोदर घाटी के बाँध नहीं होते तो 1978 के वर्ष में आसनसोल का पूरा औद्योगिक क्षेत्र दुर्गापुर, बर्दवान, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा के जिलों, जी०टी० रोड और पूर्वी रेलवे के अधिकतर भागों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचता। निचली दामोदर घाटी में जल निकासी की समस्या से इस वर्ष बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और इस दुर्घटना के लिये दामोदर घाटी निगम को जनता द्वारा जी भर कर कोसा गया था।
इसी तरह की एक घटना अगस्त 1978 में पीलीभीत (उ०प्र०) में घटी जबकि नानक सागर, कालागढ़ और बेगुलबाँध
जलाशयों से पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से रोहिलखण्ड क्षेत्र में बाढ़ का ताण्डव हुआ
जिसकी पुनरावृत्ति उन्हीं परिस्थितियों में 1986 में फिर हुई। ऐसी ही घटनायें गुजरात में (1983), महानदी-हीराकुड बाँध
(उड़ीसा-1980), वाल्वन बाँध-रायगड़ (महाराष्ट्र-1989), करन्जा बाँध (कर्नाटक-1989), मसानजोर बाँध | (पश्चिम बंगाल-1990), भाखड़ा बाँध (पंजाब-1990), में अभी हाल के वर्षों में
घटी हैं।26 वर्ष 1992 में बाँदा (उ०प्र०) की
दुर्घटना तो एकदम ताज़ी है, " ......12-13 सितम्बर, 1992 को आई भीषण बाढ़ से यहाँ ऐसी तबाही हुई वैसी पहले शायद कभी
नहीं हुई थी। लगभग 600 गावों
के लाखों लोगों की जिन्दगी को इस बाढ़ ने बर्बाद कर के छोड़ दिया। | केन नदी में, जो यमुना की एक प्रमुख
सहायक है, जल स्तर बढ़तेबढ़ते इतना
ऊँचा हो गया कि बाँदा में नदी खतरे के निशान से भी लगभग 32 फुट (10 मीटर)
ऊपर बहने लगी। नदी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि कम-से-कम 40 गावों को निगल गई और उनका
नामो निशान भी बाकी नहीं बचा।
... चार दिन तक होती रही मूसलाधार बारिश का पानी केन नदी में जाकर जमा होता रहा और जिन अधिकारियों के ऊपर नदी पर बने रंगावा व गंगाऊ बाँधों और बरियारपुर जलाशय के देख-रेख की जिम्मेदारी थी, आश्चर्य है, उन्हें खबर तक नहीं हुई। नदी के बढ़ते हुये जलस्तर व बाँध के जलाशय पर वे निगरानी रखने में एकदम असफल रहे। जब जलाशय में पानी का जमाव एकाएक एकदम बढ़ गया तो बांध के सभी द्वार एक साथ खोल दिये गये। खबर तो यहाँ तक मिली है कि जिन इंजीनियरों पर बांध की देख-रेख का भार था उनमें कोई भी ड्यूटी पर नहीं था और बांध के दरवाजे जिन लोगों ने खोले वे चपरासी थे, जिन्हें किसी तरह की कोई तकनीकी जानकारी नहीं थी। हालांकि बाढ़ निगरानी संगठनों ने जिला अधिकारों को पढ़ के आने के लगभग ५०प्टेम काढ़ की रेकी दे दी थी किन्तु फिर भी लोगों तक इसकी खबर पहुँचाने की कोई कोशिश वालों की भी है। टिहरी बाँध के उद्देश्यों के प्रति आशंका व्यक्त करते हुये प्रो० टी० शिवाजी राव कहते हैं, ‘‘किसी भी कीमत पर और जितनी जल्दी हो सके तिजोरियों को भर लेने के चक्कर में व्यवसायी वर्ग और अन्य निहित स्वार्थ वाले तत्व आम जनता के पर्यावरण संबंधी अज्ञान और नेताओं के लोभ का गलत फ़ायदा उठा कर तीसरी दुनियाँ के देशों में सरकारों को पर्यावरण की कीमत पर बड़ी सिंचाई परियोजनायें या उद्योग लगाने पर मजबूर कर रहे हैं जिसका लम्बी अवधि में नतीजा उलटा निकल रहा है। राजनेताओं और आम जनता के दिमाग में यह जबरन घुसाया जा रहा है। कि जितनी बड़ी परियोजना बनेगी उससे समाज को उतना ही ज्यादा लाभ होगा और ऐसी योजनायें आर्थिक दृष्टि से उतनी ही सक्षम होंगी। भारत जैसे देश में चुनाव जीतने और जीत कर गद्दी से चिपके रहने के लिये कुछ राजनीतिज्ञ आर्थिक सहायता के लिये ठेकेदारों पर निर्भर करते हैं और उनकी यह कोशिश रहती है कि योजना आयोग से जितना ज्यादा सम्भव हो सके योजनायें झपट कर अपने राज्य में ले जायें जबकि योजना आयोग का काम है कि उन्हीं योजनाओं को पास करे जो कि सामाजिक रूप से न्याय संगत और आर्थिक रूप से उपयुक्त हों। बड़े पैमाने पर सिंचाई और बिजली परियोजनायें हाथ में लेने से इन योजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन तथा तकनीकी उत्साह में कमी आई है। राष्ट्रीय हितों के प्रति शुरूआती दौर में राजनेताओं, अफसरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों में जो लगन रहती थी उसका स्थान अब बेसब्री और जैसे भी हो सके वैसे, मुनाफा कमाने की कोशिश ने ले लिया है। यहाँ चर्चा वैसे तो बाढ़ को लेकर हो रहा है मगर बड़े बाँधों में सिंचाई एक अहम मुद्दा होता है। उत्तर बिहार में यूँ तो बड़ा बाँध नाम की अभी तक कोई चीज़ नहीं है जिससे सिंचाई हो रही हो पर बड़ी सिंचाई योजनायें जरूर हैं। गण्डक और कोसी परियोजनायें बिहार में आज़ादी के बाद बनी हैं। कोसी परियोजना (1953) में योजना का कुल लक्ष्य 7:12लाख हेक्टेयर (17:58 लाख एकड़) था जिसे गलत और अव्यावहारिक मान कर 1975 में घटा कर 3.74 लाख हेक्टेयर (9-24 लाख एकड़) कर दिया गया था। इसी तरह गण्डक परियोजना (1964) में 10-31 लाख हेक्टेयर (25:47 लाख एकड़) ज़मीन की सिंचाई का लक्ष्य था जो कि फिलहाल 11:53 लाख हेक्टेयर (28:47 लाख एकड़) कर दिया गया है। पिछले छः वर्षों में इन योजनाओं से हुई कि योजना शुरू होने के पहले सिंचाई के बारे में जो कुछ वायदे किये गये उनके मुकाबले गण्डक परियोजना में आधी और कोसी परियोजना में महज़ चौथाई ज़मीन पर सिंचाई मिल रही है। लक्ष्यों से दूर-दूर भटकना इन बड़ी योजनाओं की त्रासदी है। यह कहना कि यह समस्या महज़ बिहार की है, बिहार के साथ नाइन्साफ़ी होगी। सिंचाई संबंधी अनुमान अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुँच पाते क्योंकि उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है।
वास्तव में सिंचाई का इन्तजाम करना एक बात हैं और उसका इस्तेमाल कर लेना एकदम अलग बात है क्योंकि इसके लिये खेतों तक नहरों का विकास और एक मज़बूत जल वितरण व्यवस्था की जरूरत पड़ती है जो कि समय पर पानी मुहय्या कर सके। संसाधनों की कभी खेतों तक नहरी पानी के न पहुँच पाने की एक खास वजह बताई जाती है और सिंचाई का प्रबन्धन, कम-से-कम बिहार में, तो ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गया है जिनकी न तो कोई जिम्मेवारी बनती है और न ही कोई जवाब देही उनके ऊपर है। समय से नहरों में पानी का न मिलना, बिना किसी सूचना के नहरों को बन्द कर देना, बिना सूचना के नहरों में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ देना, रबी के मौसम में भी नहरों को अक्सर टूटते रहना, नहरों की पेटी में बालू का जमाव, नहरी पानी में बालू की अधिकता और उसकी वज़ह से धीरेधीरे खेतों का खराब होना, पानी का रिसाव, नहरों में लाइनिंग का अभाव, और जल जमाव वगैरह कितने ही ऐसे सवाल हैं जिन पर पूरी नहर व्यवस्था और उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में तनाव बना रहता है। इनमें से एक भी मसला ऐसा नहीं है जिसको बड़े बाँध बना कर हल किया जा सके। बड़े बाँधों का निर्माण तो पूरी सिंचाई व्यवस्था को, जितना मुमकिन हो सकता है, केन्द्रीकृत करने की कोशिश है। बिहार की खुशहाली पक्की करने के लिये नेपाल में बाँधों की श्रृंखला बनाई जाने की बात आजकल जोरों पर है। अभी यदि हमारे किसान को नहर की वजह से कोई परेशानी होती है तब वह बीरपुर (कोसी हेड वर्क्स), वाल्मीकि नगर (गण्डक हेड वर्स) या फिर सोन मुख्यालय, पटना तक दौड़ जाता है और भले ही कोई सुनने वाला न हो पर उसकी हिम्मत नहीं टूटती। नेपाल में बाँध बनने पर असुविधा और अधिक बढ़ेगी यह क़रीब-क़रीब तय है क्यों कि तब फरियाद कहाँ करनी है यही तय कर पाना मुश्किल होगा। कर्नाटक और तामिल नाडु के बीच कावेरी जल विवाद का उदाहरण हमारी आँखों के सामने है मगर फिर भी वहाँ घर की बात घर में रह जाती है। नेपाली बाँधों के मामले में बात महफ़िल तक पहुँचेगी। सिंचाई की बात कहते हुये हमने जल जमाव का नाम लिया है। बिहार के कुल क्षेत्रफल 173:50 लाख हेक्टेयर में से 64-61 लाख हेक्टेयर यानी कुल ज़मीन का 37:24 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है। प्रान्त की 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर जल जमाव है। कोसी क्षेत्र में जल जमाव 182 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है।31 इसी तरह गण्डक परियोजना क्षेत्र मे 5:62 लाख हेक्टेयर जमीन खरीफ के मौसम में तथा 1.86 लाख हेक्टेयर जमीन रबी के मौसम में कुल 7:48 लाख हेक्टेयर) जल जमाव की भेंट चढ़ी हुई है।32 जबकि सच यह है कि 1992-93 में पूर्वी कोसी नहर से 177 लाख हेक्टेयर तथा गण्डक नहरों से 5:03 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हुई थी। यहाँ की बाकी नदियों के जल जमाव क्षेत्र तथा मोकामा टाल का तोहफा इन सब के ऊपर से है। गंगा के मैदानी इलाकों, खास कर उत्तर बिहार में, नहरों के पानी से पहले से ही ऊपर उठे हुये भूमिगत जलस्तर के और ऊपर उठने के खतरे साफ दिखाई पड़ते हैं। ऐसी जगहों पर उन नहरों की जरूरत एकदम नहीं है जो कि सिर्फ बरसात में पानी देकर बाढ़ और जल जमाव की समस्या को और भी गम्भीर बनाती हैं। सारण जिले के गरखा प्रखण्ड की कोठिया और हसनपूरा पंचायत में गाँव वालों ने गण्डक परियोजना की नहरों को काट-काट कर जमीन में मिला दिया है क्योंकि इन नहरों से पानी नहीं मिलता था और बरसात के पानी का रास्ता रोक कर यह नहरें जल-जमाव में वृद्धि करती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि गण्डक नहरों से जितनी सिंचाई होती है उससे ज्यादा उस इलाके में जल जमाव है। यही स्थिति कोसी नहरों की भी है। बड़ी-बड़ी नहरें बना कर और लाइनिंग किये बिना उनका इस्तेमाल करना जल जमाव को दावत देना है। ऐसा करने से खेती का रकबा कम होता है और यह हो भी रहा है। पूर्वी कोसी नहर क्षेत्र में भी कितनी ही ऐसी नहरें हैं जिनमें आज तक एक भी बूंद पानी नहीं आया और न ही आने की कोई उम्मीद है क्योंकि नहरों के तल के ढाल उल्टे हैं।

जल जमाव सिर्फ खेती का रकबा ही कम नहीं करता वह छोटे और
सीमान्त खेतिहरों को भूमिहीन बनाता है और रोजी-रोटी की तलाश में बाहर भटकने को
मजबूर करता है। अपनी जरूरत भर अनाज पैदा कर पाने वाले किसानों को मजदूर बनाता है।
खेतों को तालाब बनाता है और अनाज की जगह मछलियाँ, केकड़े और घोंघे पैदा करता है। सड़क पर चलने वाली जीप, ताँगा, बस, साइकिल जैसी सवारियों की
जगह लोगों को नाव खेने पर मजबूर करता है। घरों की मिट्टी की दीवारों को बाँस/लकड़ी
में तबदील करता है। कालाजार, जापानी
इसीफिलाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाता है। पति के जिन्दा रहते हुये
महिलाओं को विधवा की तरह जीने के लिये मजबूर करता है और मासूम बच्चों को पिता के
प्यार और अनुशासन से वंचित रखता है। पूरी स्थानीय उत्पादन प्रक्रिया को चौपट करके
इलाके के बाशिन्दों को एक कभी भी खतम न होने वाले मनीऑर्डर के इन्तजार में ढकेलता
है जो कि उसके अपने लोग पंजाब, हरयाणा, गुजरात, नेपाल, बंगाल या ऐसी ही अन्य
जगहों से भेजते हैं। यानी अकेला जल जमाव इलाके की पूरी की पूरी जीवन पद्धति को तहस
नहस कर डालता है। पहले जैसा कुछ भी बाकी नहीं बचता। इन हालात से निबटने में लम्बा
अरसा लगता है और इसका कोई बना बनाया हल अभी तक नहीं है। बड़े बाँध और उनसे होने वाली
सिंचाई जल जमाव की समस्या को बदतर बनायेंगे और यह एक इतिहास सिद्ध तथ्य है।
इसके अलावा बड़े बाँधों की समस्यायें यहीं आकर समाप्त नहीं होतीं। ऐसी उपयुक्त जगहें जहाँ इस तरह के बाँध बनाये जा सकते हैं एक-आध ही होती है और एक बार इन का इस्तेमाल कर लिये जाने के बाद फिर दूसरी जगहें नहीं बचतीं जहाँ इनका निर्माण किया जा सके। इसके अलावा अगर नदी का बहुत अधिक जल ग्रहण क्षेत्र बाँध के नीचे है तब भी बाढ़ की स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाँध के पीछे टिके हुये पानी में जमा होती हुई रेत/मिट्टी जलाशय के जीवन काल को घटाती है और उसके साथ-साथ जमा हुआ पानी आस-पास के वातावरण के तापक्रम में फेर बदल करता है और नमी फैलने के कारण नये-नये कीड़े-मकोड़े और जीवाणु पैदा होते हैं जो कि नये किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं। जलाशय के पानी का लगातार भाप बन कर उड़ते रहने के कारण जलाशय में रसायनों की सघनता बढ़ती है और यह पानी जिस किसी इस्तेमाल में लाया जाता है उस पर इन रसायनों का असर पड़ता है।
तटबंध
बाढ़ से बचाव का
दूसरा तरीका नदी के किनारे तटबन्ध बना कर उन इलाकों की हिफाजत करना है जिनमें नदी
का पानी फैल जाया करता है। बाढ़ों से बचाव के लिये नदियों पर तटबन्ध बनाना शायद
सबसे पुराना तरीका है। मिस्र की नील नदी पर बारहवीं शताब्दी में तटबन्ध बनाये गये
थे और बेबीलोन शहर के बाढ़ से बचाव के लिये भी तटबन्धों का निर्माण किया गया था।
चीन की हाँगो नदी पर तटबन्धों का निर्माण ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में शुरू हो
गया था जबकि यॉग्सी नदी पर तटबन्ध पहली शताब्दी में बने थे। चीन में तटबन्धों
द्वारा इस शताब्दी के मध्य तक 22 प्रान्तों
की लगभग 56 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि
को बाढ़ से सुरक्षा मिलती थी और वहाँ की तकरीबन आधी आबादी इन तटबन्धों के पीछे
पनाह लेती थी। जापान में भी बाढ़ वाले इलाकों को बचाने के लिये तटबन्धों का
इस्तेमाल हुआ है। इटली की पो नदी के तटबन्ध बाढ़ सुरक्षा देने के लिये काफी मशहूर
रहे हैं और अमेरिका की मिस्सीसिपी नदी के तटबन्ध 1727 में बनाकर पूरे कर लिये गये थे।
बिहार में तटबन्धों का जो इतिहास उपलब्ध है उसके हिसाब से पहला तटबन्ध कोसी नदी के किनारे बारहवीं शताब्दी में बना था। बीर बाँध नाम के इस तटबन्ध के निशान अभी भी बीरपुर (सुपौल) के पास दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद गण्डक नदी पर बने तटबन्धों का जिक्र आता है जो कि अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्य में बने थे। तब से आजादी तक बहुत से तटबन्ध जमींदारों द्वारा बनवाये गये। बहुत से इन्जीनियरों का यह मानना है कि प्राचीन काल में बने तटबन्धों में आज की वैज्ञानिक क्षमता का अभाव था और वे उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाते थे जितनी कि उनसे उम्मीद की जाती थी और उनके टूटने की वजह से तबाहियाँ बरकरार रहती थीं। इस वजह से जहाँ एक ओर तटबन्धों के हिमायती उनकी वकालत करते नहीं अघाते थे वहीं उनके मुखालिफों की भी कमी नहीं थी। इस बहस में पड़ने के पहले हम तटबन्धों के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेंगे। नदियों के पानी के फैलाव को रोकने और गाँवों/बस्तियों को बाढ़ के पानी से बचाव के लिये नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनाये गये हैं। इन तटबन्धों की मौजूदगी का असर नदी के प्रवाह, आस-पास के इलाकों से बह कर नदी में आने वाले पानी, भूमिगत जल, समेत जिन्दगी के बहुत से पहलुओं पर पड़ता है। इनमें से कुछ पहलुओं पर हम जरा विस्तार से चर्चा करेंगे।

नदी पर तटबन्ध बनने के बाद की स्थिति को दिखाया गया है। बाढ़ के समय नदी में होकर बहने वाले पानी को फैलने से रोकने के लिये तटबन्धों के बीच का फासला इंजीनियरों द्वारा डिजाइन कर के निर्धारित किया जाता है। इसमें निश्चित तौर पर कुछ गाँव तटबन्धों के अन्दर फँस जाते हैं। तटबन्ध बनने की वजह से नदी का पानी पहले जितना फैल नहीं पाता जिसके नतीजतन तटबन्ध के अन्दर जो भी गाँव पड़ते हैं उनको पहले के मुकाबले बाढ़ के थपेड़े ज्यादा झेलने पड़ते हैं। दूसरी बात यह कि बाढ़ के पानी के साथ एक बड़ी मात्रा में रेत/मिट्टी बह कर आती है जो कि पहले की तरह बड़े इलाके पर फैल नहीं पाती और धीरे-धीरे तटबन्धों के अन्दर जमा होती रहती है। इससे नदी का तल उसी गति से ऊँचा उठने लगता है और पानी के बहाव के लिये नदी में जगह कम होने लगती है। इस स्थिति से निबटने के लिये तटबन्धों को ऊँचा करना पड़ता है। आज से लगभग 2,500 साल पहले बने चीन की ह्वाँग हो नदी । के तटबन्धों को बहुत ज्यादा ऊँचा करना पड़ा है। इस नदी में मिट्टी/रत के जमाव की दर 1 से०मी० से 10 से०मी० प्रति वर्ष तक देखी गई है जिसकी वजह से नदी का तल कुछ स्थानों पर आस-पास की जमीन से 10 मीटर . तक ऊपर है।

चौथी बात यह कि जहाँ दो धाराओं का संगम होता है वहाँ अगर मुख्य नदी पर तटबन्ध बने हों तो सहायक नदी का मुँह बन्द हो जायगा और तब इस नदी का पानी या तो पीछे की ओर फैलेगा या तटबन्धों के साथ-साथ बहने लगेगा। यह हालत गैर मुमकिन नहीं है। कमला बलान नदी इसकी नजीर है जो कि मधुबनी जिले में कभी भेजा के पास बकुनियाँ गाँव में कोसी से मिलती थी । कोसी पर जब पचास के दशक में तटबन्ध बना तो कमला बलान का मुहाना बन्द हो गया और अब यह नदी कोसी के साथ-साथ काफी दूर तक बहती है और मधेपुर (मधुबनी) के दक्षिण दरभंगा जिले के घनश्यामपुर, बिरौल और कुशेश्वर स्थान प्रखण्ड तथा सहरसा के महिषी प्रखण्ड के पश्चिमी हिस्से की तबाही का सामान बनती है।

ऐसी हालत में नदियों के संगम स्थल पर स्लुइस गेट बनाने की बात उठती है जिससे सहायक धारा के पानी को नियंत्रित कर के बड़ी नदी में छोड़ा जा सके। मगर मुसीबत यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। होता यह है कि तटबन्ध के भीतर नदी में मिट्टी/रेत जमा होती रहती है और यह स्लुइस गेट के मुँह को जाम करती है। शुरू के कुछ साल तो सफाई वगैरह चलती रहती है पर उसके बाद जब जोश ठण्डा पड़ जाता है तब स्लुइस गेट नदी के बालू में करीब-करीब दफ़्न हो जाता है। स्लुइस गेट का जाम होना वैसे एक बहाना ही है। अगर बड़ी नदी में बाढ़ उसकी सहायक नदी से ज्यादा है तो स्लुइस गेट खोल के नहीं रखा जा सकता क्योंकि तब पानी उलटा छोटी नदी में बहने लगेगा और नये-नये इलाकों में बाढ़ लायेगा और अगर स्लुइस गेट को बन्द रखा जाय तो सहायक धारा का पानी बाहर फैलेगा। बाढ़ दोनों ही हालत में आयेगी मगर बाढ़ से बचाव की मृग नृष्णा स्लुइस गेट बनवाती है और जब इससे भी बचाव नहीं होता तब सहायक धारा पर भी तटबन्ध बना देने की बात उठती है और कोई चारा न होने पर यह फर्ज तटबन्ध का टूटना कोई अनहोनी नहीं है। ज्यादा पानी आने पर नदी का पानी तटबन्ध के ऊपर होकर बह सकता है या फिर अत्यधिक रिसाव या सीपेज (Seepage) के कारण भी तटबन्ध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। तटबन्धों के टूटने का तीसरा कारण नदी की टेढ़ी-मेढ़ी बहती हुई धाराओं द्वारा किये जाने वाला कटाव है।

कटाव रोकने के लिये तटबन्धों से समकोण बनाते हुये नदी के अन्दर की दिशा में बाँध बनाये जाते हैं जिन्हें स्पर (Spur) कहते हैं। इन स्परों के निर्माण से नदी की धारा को तटबन्धों के बीच में रखने में मदद मिलती है। बहुत ज्यादा कटाव की हालत में पहले स्पर कटता है और इसके बाद ही नदी तटबन्ध पर हमला कर पाती है। इसके अलावा तटबन्ध के स्लोप पर पत्थर की पिचिंग, लकड़ी के बल्लों की बाड़ बना कर उनके बीच पत्थरों को भर कर स्परों की तरह इस्तेमाल करना, तार की जाली में बाँध कर ईंट और पत्थरों की मदद से कटाव रोकना और जब कुछ भी न बन पड़े और यह जाहिर हो जाय कि तटबन्ध को इस साल की बाढ़ में टूटने से नहीं बचाया जा सकता तब पहले से ही एक दूसरा तटबन्ध बनाकर रखना जिससे बाढ़ का पानी इस नये तटबन्ध से आगे न जा पाये । तकनीकी भाषा में इस दूसरे तटबन्ध को निवृत्त रेखा तटबन्ध (Retired Line Embankment) कहते हैं।

अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बार जिस जगह रिटायर्ड लाइन बन
गई। वहाँ यह सिलसिला शुरू हो जाता है और एक के बाद एक कई रिटायर्ड लाइनें बनती हैं
जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है। इन रिटायर्ड लाइन तटबन्धों की जद में अक्सर वह
गाँव या बस्तियाँ हँसती हैं जो कि तटबन्ध से बाहर होने के कारण शुरू-शुरू में
सुरक्षित मानी जाती थीं फिर तटबन्ध के नजदीक होने के कारण पहले तो जल जमाव की चपेट
में आती हैं फिर तटबन्ध टूटने के आतंक के साये में जीती हैं और कभी-कभी तटबन्ध टूट
भी जाता है। तटबन्ध अगर न भी टूटे तो कई मामलों में टूटने का खतरा कम करने के लिये
रिटायर्ड लाइन तटबन्ध के निर्माण से पैदा हुई बदनसीबी उन्हें तटबन्धों के अन्दर
खींच ले जाती है।
गाँवों को ऊँची जगह पर बसाना
बाढ़ वाले इलाके में गाँव वैसे भी ऊँची जगहों पर ही विकसित
होते हैं। इसकी एक वजह यह है कि बाढ़ों की वजह से घर गिरते रहते हैं और नया घर
अक्सर पुराने घर के मलवे पर बनाया जाता है। हमने पहले थोड़ा इशारा किया था कि बाढ़
वाले इलाकों के गाँवों में जाने के लिये गर्मी के दिनों में भी नाव की जरूरत पड़
जाया करती है। ऐसे गाँवों में बरसात के मौसम में पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा हो
जाता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है।
गाँवों को नये सिरे से जब टीलों पर बसाने की कोशिश होती है तब एक तो खेत पानी में डूबे रह जाते हैं जिससे कि जिन्दगी गुजारने के लिये अनाज का उत्पादन अगर बिल्कुल खतम न हो तब भी कम जरूर हो जाता है क्योंकि बरसात वाली फसल निश्चित तौर पर मारी जाती है। दूसरी दिक्कत | यह है कि गाँव को जब मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाता है, और इसके बिना काम चल नहीं सकता, तो बहते पानी के अन्दर यह पूरी संरचना स्पर की तरह से सलूक करने लगती है जिससे इसके खुद के ऊपर कटाव का खतरा पैदा हो जाता है। यह खतरा मुख्य सड़क से दूर वाले किनारे पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वह जगह बहते पानी के सीधे सम्पर्क में आती है। तीसरी परेशानी यह है कि गाँव काफी ऊँचा बस जाने पर उस में सामान या लदी हुई बैलगाड़ी आदि ऊपर तक पहुँचाने में दिक्कत होती है। कभीकभी ज्यादा ऊपर रहने वाले गृहस्थों को अपने मवेशी, गोदाम वगैरह निचले इलाकों में रखने पड़ते हैं।

मगर रिंग बाँधों के साथ भी बाढ़ के पानी के साथ आई मिट्टी और रेत वही सलूक करती है जो कि तटबन्धों के मामले में देखने आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह रेत/मिट्टी रिंग बाँध के बाहर जमा होना शुरू होती है जिससे कि रिंग के बाहर जमीन का तल ऊपर उठना शुरू होता है और रिंग बाँध की प्रभावी ऊँचाई साल दर साल कम होना शुरू होती है और फिर दस्तूर के मुताबिक रिंग बाँध की ऊँचाई बढ़ाने की माँग उठती है। अब रिंग बाँध की ऊँचाई जितनी बढ़ाई जायेगी उतना ही बचाव किया जाने वाला गाँव/शहर पहले के मुकाबले ज्यादा गड्ढे में चला जायगा। अब अगर यह रिंग बाँध कभी टूट जाय तो बाहर बहता हुआ सारा पानी रिंग बाँध के अन्दर घुस जायेगा और पहले से कहीं ज्यादा तबाही का सामान बनेगा।

बिहार के भूतपूर्व मुख्य अभियंता कैप्टेन जी० एफ० हॉल (1937) ने कहा था कि नदियों के दोनों किनारों पर बने तटबन्ध एक न एक दिन आकार में इतने बड़े कर देने पड़ेंगे कि इनका रख रखाव असम्भव हो जायेगा और वे टूटेंगे और आस-पास के स्थानों की पूरी तबाही का सामान बनेंगे। यदि वे बस्तियों की सुरक्षा के लिये घेरे के रूप में प्रयोग किये जायें तो वे सुरक्षित स्थान को दल-दल में परिवर्तित कर देंगे जिसके चारों ओर भूमितल ऊपर होगा और तब यदि रिंग बाँध टूटता है तो तथाकथित सुरक्षित इलाके की जो दुर्गति होगी उससे कहीं बेहतर असुरक्षित क्षेत्र होंगे। रिंग बाँध टूटने की बात को फ़िलहाल एक अतिवादी चिन्तन कह कर टाला जा सकता है क्योंकि अभी तक बिहार में ऐसी घटना हुई नहीं है पर यह सच है कि निर्मली में बरसात के पानी की निकासी के लिये 49 हॉर्स पॉवर के तीन पम्प बैठाये गये थे जिनमें से अब एक पम्प का तो पम्प हाउस समेत नामो निशान मिट गया, दूसरे पम्प हाउस का महज़ प्लेट फॉर्म बाकी है और सिर्फ तीसरा पम्प काम करता है जिसका कि स्लुइस गेट 1980 में जुलाई महीने के आखिर तक तकनीकी गड़बड़ी के कारण बन्द नहीं हो पाया और नदी का पानी कस्बे में घुस गया था। असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया शहर इसी तरह के रिंग बाँधों के बीच आबाद है। वहाँ लगभग हर साल बचाव के लिये सेना को उतारना पड़ता है। पानी की निकासी की गंभीर समस्या, जल जमाव, कीचड़ और मच्छरों का आतंक अब निर्मली के पर्याय हैं। आजमगढ़ और जौनपुर में अभी यह समस्या उतनी गंभीर नहीं हुई है मगर रिंग बाँध के अन्दर बढ़ते हुये शहरी विकास को देख कर भविष्य के प्रति आशंका जरूर बढ़ती है। कैप्टेन हॉल के कथन में भी इस आशंका की पुष्टि होती है। उन्होंने कहा था कि ... इन मायावी सुरक्षा साधनों से तथा कथित सुरक्षित लोग हमेशा तटबन्ध की ऊँचाई बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने की माँग करते रहेंगे जब कि उन्हें यह पता नहीं होगा कि इससे समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी और (ऐसा करने से) उनकी जमीन और अधिक नीची होती चली जायेगी और प्रलय का वक्त कुछ दिनों के लिये और टल जायेगा। बिहार में कभी-कभी ‘छोड़ो नदी और बांधो गाँव' जैसे नारे सुनाई पड़ते हैं और यह आशा की जाती है कि इस माँग की सीमायें समझने में कैप्टेन हॉल के कथन से जरूर मदद मिलेगी। 2.5 नदी को चौड़ा और गहरा करना जन साधारण में बाढ़ से बचाव के इस तरीके का चर्चा आम होता है, और यह सच भी है कि नदियों को अगर गहरा और चौड़ा कर दिया जाय तो उनमें पानी बहने की क्षमता बढ़ जायगी और इलाके में बाढ़ घट जायेगी। सरसरी तौर पर यह बात एकदम दुरुस्त लगती है। मगर पानी के साथ मिट्टी/रत की मात्रा की कल्पना से यह तरीका भी अव्यावहारिक लगने लगता है। नदियों को चौड़ा और गहरा करने के सन्दर्भ में अगर कोसी का उदाहरण लें तो उसमें लगभग 11,100 हेक्टेयर मीटर रेत/मिट्टी प्रति वर्ष आती है। इतनी मिट्टी से अगर 1 मीटर चौड़ा) x1मीटर (ऊँचा) बाँध बनाया जाय तो वह भूमध्य रेखा के तीन फेरे लगायेगा, नदियों की जब डिसिल्टिंग की बात उठती है तो हमें इतने ही परिमाण में मिट्टी की कटाई/ढुलाई के बारे में सोचना होगा। जैसा कि हम पहले कह आये हैं, महिषी से कोपड़िया की 33 कि० मी० की दूरी के बीच नदी तटबन्धो में लगभग 12 से० मी० प्रतिवर्ष की दर से कोसी का तल ऊपर उठ रहा है। यदि तटबन्धों के बीच की दूरी औसतन 10 कि० मी० मान ली जाय तो लगभग 39:6x106 घन मीटर सिल्टरित इसमें हर साल जमा होती है जो कि 66 लाख ट्रक मिट्टी के बराबर बैठती है जिसे नदी के तल को आज के स्तर पर बनाये रखने के लिये हर साल हटाना पड़ेगा। अगर मिट्टी काटने का यह काम हर साल 15 दिसम्बर से 15 मई के कार्यकारी मौसम में किया जाय तो रोज़ साइट पर लगभग 37,000 ट्रक मिट्टी ढोने के लिये चाहिये।

और इतने ट्रकों को अगर एक लाइन में एक दूसरे से सटा कर खड़ा कर दिया जाय तो ट्रकों का दूसरा छोर लगभग 260 कि०मी० की दूरी पर दिखाई देगा। इतनी मिट्टी को केवल काट कर ट्रक में रखने का खर्च 46 करोड़ रुपये सालाना आयेगा जबकि बिहार सरकार एक साल में चालीस करोड़ रुपये के आसपास पूरे प्रान्त के बाढ़ नियंत्रण पर खर्च करती है। करीब-करीब इतनी ही मिट्टी बीरपुर बराज और महिषी के बीच से निकलेगी। फिर कोसी अकेली नदी तो है नहीं। उत्तर बिहार में इसके अलावा गण्डक, बूढ़ी गण्डक, बागमती, अधवारा समूह, कमला तथा महानन्दा की घाटियाँ भी पड़ती हैं। इतनी मिट्टी लेकर हम कहाँ जायेंगे। इसका एक तैयार जवाब है कि यह मिट्टी चौरों में डाल दी जायगी। अब प्रश्न है कि कौन-सा किसान अपनी ज़मीन पर बालू डलवाने को तैयार होगा और यदि सारे चौर भर डाले गये तो उसका जल निकासी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। अगर उत्तर बिहार की नदियों की डिसिल्टिंग हाथ में ले भी ली जाय तो क्या गंगा की चौड़ाई या गहराई बढ़ाये बिना कोई लाभ होगा क्योंकि अन्ततः यह नदियाँ गंगा में ही जाकर मिलती हैं। केवल उत्तर बिहार की नदियों की खुदाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और अगर गंगा की खुदाई शुरू की जायगी तो फरक्का बराज का क्या होगा जो कि डिसिल्टिंग या खुदाई की राह का रोड़ा बनेगा और जब तक यह बराज रहेगा गंगा की डिसिल्टिंग का कोई मतलब नहीं होगा। अगर फरक्का से भी फुर्सत पा ली जाय तो फरक्का के आगे चल कर गंगा के दो भाग हो जाते हैं। एक हिस्सा पद्मा के नाम से बांग्लादेश की ओर जाता है और दूसरा भागीरथी/हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाता है। पद्मा की डिसिल्टिग हमारे हाथ में नहीं है, पर भागीरथी की डिसिल्टिंग हम जरूर कर सकते हैं। ऐसा करने पर भागीरथी में पानी का प्रवाह बढ़ेगा और वह फिर एक राजनैतिक परेशानी पैदा करेगा क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही फरक्का में गंगा के पानी पर अपना दावा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। फिर अगर किसी तरह से समुद्र तक डिसिल्टिंग कर भी ली जाय तो नदी और समुद्र के संगम स्थल पर नदी का और समुद्र का लेवेल एक सन्तुलन की स्थिति में है जिसमें केवल अस्थायी परिवर्तन आयेगा और दो एक साल बाद हालत पुरानी स्थिति में लौट आयेगी।

इसके अलावा इतने बड़े काम के लिये धन कहाँ से आयेगा। यदि
यह काम मशीनों से करना है तो मशीनों की खरीदारी, संचालन, और रख
रखाव पर कितना पैसा खर्च होगा । इन सब कारणों से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) भी इस तरीके से बाढ़
नियंत्रण के हक में नहीं है। प्रधानमंत्री 1993 में अगस्त माह के अन्त में जब बिहार आये थे तो उन्होंने नदियों की
डिसिल्टिंग करके बाढ़ों के प्रभाव को कम करने पर बल दिया था। बाढ़ों पर डिसिल्टिंग
का क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो कह पाना मुश्किल है पर इससे मिट्टी के काम में लगे
ठेकेदारों और ट्रक मालिकों को जरूर लाभ पहुँचेगा।
यह काम तो छोटी मोटी नदियों पर सम्भव है जिनके पानी में
मिट्टी/ रेत की मात्रा बहुत कम है। इन छोटी नदियों की खुदाई पर भी हाथ लगाने पर
सारे पुलों को फिर से बनाना या विस्तार करना पड़ेगा और खुदी हुई मिट्टी/रेत को
किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। इसके बावजूद दोतीन बरसातें काफी है कि
मिट्टी/रेत का बेताल फिर पेड़ पर जा बैठे। हिमालय और गंगा घाटी की नदियों के
सन्दर्भ में बाढ़ से बचाव के इस तरीके का चर्चा भी नहीं होता क्योंकि इसकी खामियों
से सभी वाकिफ हैं।
जल मार्गों में सुधार
भारी मात्रा में रेत/मिट्टी से लदी नदियाँ जब मैदानों में
उतरती हैं तो उनकी धारायें बलखाती हुई चलती हैं। कभी-कभी एक ही नदी की कई धारायें
बन जाती है जो कि आपस में मिलती बिछुड़ती रहती हैं। कभी-कभी नदी महज एक नदी न रह
कर ऐसी कई धाराओं का समूह बन जाती है। नदियों के इस तरह के व्यवहार का कारण उनमें
मिट्टी/रेत का अधिक होना ही होता है। पानी भी कभी किसी धारा में तो कभी किसी धारा
में ज्यादा प्रवाहित होता है।
नदियों के घुमावदार प्रवाह से कटाव और जल जमाव दोनों की ही समस्यायें सामने आती है। उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बड़े-बड़े चौरों का होना इसका प्रमाण है। ऐसी मान्यता है कि पश्चिम में गंडक नदी की धारा में परिवर्तन की वजह से इन चौरों का निर्माण हुआ तो पिछले दो सौ वर्षों में पूणियाँ के पूर्व से कोसी के लगभग 160 कि०मी० पश्चिम दरभंगा/मधुबनी से होकर बहने के कारण पूर्णियाँ, सहरसा में चौरों का निर्माण हुआ। कमोबेश यही हालत पूर्व में करतुआ, तीस्ता से लेकर पश्चिम में शारदा नदी तक है। जिसमें नदी द्वारा छोड़े गये मार्ग में चौरों का निर्माण तथा कटाव के कारण धाराओं के सीधा होने तक की प्रक्रिया को समझाया गया है।

नदी के प्रवाह पथ को सीधा कर देने पर (चित्र 2.9) उसका रास्ता छोटा हो जाता
है और उसके तल के ढलान में अचानक वृद्धि के कारण पानी की रफ्तार तेज हो जाती है
जिससे ठीक सामने पड़ने वाली बस्तियों पर कटाव का खतरा पैदा हो सकता है। राष्ट्रीय
बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट में भी इस
तरीके के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता । आयोग लिखता है--"... नदी के टेढ़े मेड़े मोड़
के साथ-साथ काटें बना कर जलमार्ग को सीधा और कम करना खतरे का काम है क्योंकि काट
(कट ऑफ) के अनुप्रवाह में बाढ़ के स्तर में तत्काल वृद्धि हो सकती है और काट के
क्षेत्र में नदी के पानी का वेग प्रेरित हो सकता है जिससे आखिरकार तल कटाव की
गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। फिर भी, सभी
आकारों की नदियों के जलमार्ग के सुधार के लिये विवेकपूर्ण ढंग से आयोजित की गई
काटों का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है।''
इस प्रकार नदियों के घुमावदार मार्गों को सीधा करना भी बाढ़
से मुक्ति पाने का आसान उपाय नहीं बनता।
एक नदी के पानी को दूसरी नदी में डालना या दूसरे मार्ग से वापस उसी नदी में पहुँचाना
कभी-कभी कम पानी
वाली नदी में अधिक प्रवाह वाली नदी के पानी को मोड़ना बाढ़ से बचाव का एक तरीका हो
सकता है। बदनसीबी से गंगा घाटी की नदियों में इस तरह की सहूलियत नहीं है। यहाँ जब
बाढ़ आती है तब तकरीबन सारी नदियाँ भरी रहती हैं। वैसे भी यह काम पहाड़ी इलाकों
में सुरंगों के जरिये किया जाता है। गंगा घाटी के पहाड़ी इलाके ज्यादातर नेपाल में
पड़ते हैं जिन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। यूँ भी यह तरीका बहुत ही खर्चीला है
और तराई समेत गंगा के मैदानी इलाकों में आबादी की सघनता को देखते हुये मुमकिन नहीं
जान पड़ता । यद्यपि इस तरीके से बाढ़ से बचाव की एक कोशिश हमारे देश में सन् 1872 में उड़ीसा में महानदी के
15 लाख घनसेक (42,505 घनमेक) प्रवाह में से 11 लाख घनसेक (3117 घनमेक) प्रवाह को बिरूपा
नदी के माध्यम से ब्राह्मणी नदी में छोड़ कर की गई थी। इसी तरह आजादी के आस-पास
आंध्रप्रदेश में बुडामेरू नदी के कुछ पानी को कृष्णा नदी में छोड़ा गया था।41 पर यह इसलिये सम्भव हो
सका था कि रास्ते में इस बदलाव से किसी अतिरिक्त तबाही का अंदेशा नही था।
एक ही नदी के पानी के कुछ हिस्से को. घुमावदार रास्ते से ले
जाकर नीचे उसी नदी में छोड़ने पर बाढ़ के प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है
क्योंकि घुमाये गये पानी को अब वापस नदी में पहुँचने में पहले से ज्यादा समय
लगेगा। इस तरह का एक प्रयास बिहार में सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर किया जा
रहा है। देवापुर के पास बेलवाधार से होकर 50,000
घनसेक (1559 घनमेक) का प्रवाह बागमती की मुख्य धारा से अलग करके फिर
कलंजर घाट के पास उसी नदी में मिलाने की कोशिश चल रही है जिससे बागमती में आने
वाले सर्वाधिक डिस्चार्ज की रफ्तार को उसी अनुपात में कम किया जा सकेगा क्योंकि
बेलवाधार से होकर कलंजर घाट तक वापस बागमती पहुँचने वाले पानी को लगभग 72 घण्टे का समय लगता है
जबकि बागमती से सीधे कलंजर घाट पहुँचने वाले पानी को 56 घण्टे का समय लगता है। इस तरह 50,000
घनसेक (1559घनमेक) पानी 16 घण्टे
देर से कलंजर घाट पहुँचेगा और बाढ़ को उसी अनुपात में कम किया जा सकेगा। | यह एक अलग बात है कि
पिछले लगभग 15 वर्षों से चल रही यह
कोशिश अभी तक नाकाम साबित हुई है।
डिटेन्शन बेसिन
आमतौर पर बलुआही जमीन के इलाकों में नदियों के कगार आसपास
की जमीन से ऊपर उठे हुये होते हैं। इन उठे हुये कगारों की वजह से जहाँ एक ओर इलाके
के चौरों का पानी नदी में वापस नहीं जा पाता वहीं बरसात के दिनों में कगारों को
तोड़ कर बहती हुई नदी इन चौरों को भर देती है और यह पानी फिर नीचे कहीं और जाकर
नदी में मिलता है। इस प्रकार बाढ़ का कुछ नियमन तो अपने आप ही हो जाता है।
जहाँ यह काम नदी खुद नहीं कर पाती वहाँ तकनीकी व्यवस्था कर के उसे ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है कि उसका पानी इस प्रकार की प्राकृतिक झीलों में चला जाय। इन झीलों या चौरों को डिटेन्शन बेसिन कहते हैं क्योंकि नदी के अतिरिक्त पानी को अब Detain या रोक कर रखा जाता है। ऐसा करने से नदी के पानी में आये भारी बालू व मिट्टी के कणों को चौरों में बैठने का भी मौका मिल जाता है और चौरों से नीचे बहने वाला पानी अपेक्षाकृत साफ होता है। यानी उसमें पहले के मुकाबले मिट्टी/रेत के कण कम होते हैं। जाहिर है यह पानी जब फिर नदी की धार में नीचे वापस आयेगा तब उसकी मिट्टी/रेत बहा ले जाने की क्षमता पहले के मुकाबले ज्यादा होगी जिससे नदी की तलहटी की बेहतर सफाई हो जाती है तथा इस डिटेन्शन बेसिन का एक फायदा और होता है कि चौर धीरे-धीरे भर जायगा और कुछ वर्षों बाद उनमें खेती के लायक उपजाऊ जमीन निकल जायगी । बाढ़ नियंत्रण का यह सबसे आसान, कारगर और कम खर्चीला | तरीका है। दुर्भाग्यवश गंगा घाटी में इस तरह के चौर हैं तो जरूर मगर ऐसे नहीं हैं कि जो गंगा या उसकी खास-खास सहायक धाराओं के पानी के रेले को सम्भालने में कारगर साबित हो सकें। इसलिये इस तरीके से भी बहुत ज्यादा भले की उम्मीद करना मायूसी को ही न्यौता देना होगा।