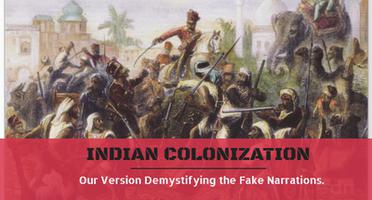महानंदा नदी अपडेट - बिहार,बाढ़ और महानंदा
- By
- Dr Dinesh kumar Mishra
- September-25-2018
बिहार–गौरवशाली अतीत
भारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा जब भी होती
है, तो सबसे पहले बिहार का नाम लिया जाता है। देवताओं और दानवों ने मिलकर जब
समुद्र मंथन किया था। तब मन्दार पर्वत ही समुद्र को मथने के लिये प्रयुक्त हुआ था।
यह स्थान वर्तमान भागलपुर जिले में पड़ता है, हो सकता है उस समय समुद्र की सीमायें यहाँ तक रही हों। इस
क्षेत्र के उत्कर्ष की कहानियाँ राजा जनक के काल से सुनने को मिलती हैं। याज्ञवल्क, गौतम, च्यवन, श्रृंग, विश्वामित्र, अष्टावक्र, कात्यायन, पतंजलि, वर्ष, उपवर्ष, पाणिनी, अश्वघोष, वात्स्यायन, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जैसे विद्वानों
और शिल्पियों से बिहार आदिकाल से गौरवान्वित होता रहा है। मिथिला प्राचीन काल में
संस्कृति, शिक्षा, कला और साहित्य का एक बहुत बड़ा केन्द्र
था जिसने देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। भगवान
महावीर ने इसी धरती से सारी दुनियाँ को प्रेम, करुणा, सौहार्द और सहिष्णुता का उपदेश दिया।
यहीं राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने जिनके वचनामृत का प्रचार-प्रसार सारे
विश्व में हुआ।
वाल्मीकीय रामायण में भगवान राम का विवाह
के उद्देश्य से अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुध्रन के साथ जनकपुर जाने का वृतान्त मिलता है।
इस यात्रा में उन्होंने बक्सर के पास ताड़का वध किया था तथा सिद्धाश्रम, अहिल्या-आश्रम, गौतम आश्रम और वैशाली होते हुए जनकपुर की
यात्रा तय की थी। महाभारत काल के समय जरासन्ध की राजधानी वर्तमान राजगृह और कर्ण
के अंग देश की राजधानी वर्तमान चम्पानगरी (भागलपुर) में थी। पाण्डवों के वनवास तथा
अज्ञातवास का काफी समय पूर्णियाँ के जंगलों में बीता। भीम ने कभी मोदागिरि
(वर्तमान मुंगेर) पर विजय पाई थी तथा खड़गपुर हवेली के पास स्थित भीम बाँध का संबंध
भीम से माना जाता है।
सोनपुर (छपरा) के पास के हरिहर क्षेत्र
के साथ भी कहा जाता है कि पशुपति नन्दी के नेतृत्व में एक बार भगवान विष्णु यहाँ
बहुत सी गायों को साथ लेकर आये थे। जिसके कारण इस स्थान का नाम हरिहर क्षेत्र
पड़ा। इसी स्थान पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी जबकि गज की रक्षा के लिये स्वयं
भगवान विष्णु को नंगे पैर, बिना गरुड़ की सवारी के आना पड़ गया था।
ऐतिहासिक काल में बिहार का वर्णन संभवतः मगध के बिम्बसार (छठी शताब्दी ई० पू०) से शुरू होता है और ऐसी मान्यता है, कि इसी काल में भगवान वर्द्धमान महावीर और भगवान बुद्ध का अभ्युदय हुआ। लगभग इसी समय वैशाली में लिच्छवी राजत्व अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा था। नन्द वंश के पतन के साथ मगध में 321 ई० पू० में चन्द्र गुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना हुई जो कि उत्तर में हिन्दुकुश से लेकर दक्षिण में तन्जावुर तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में हुगली तक फैला हुआ था। चन्द्र गुप्त मौर्य के उत्थान में चाणक्य (कौटिल्य) की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चाणक्य स्वयं किस स्थान के रहने वाले थे इसमें कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग उन्हें तक्षशिला का निवासी मानते हैं जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार चाणक्य वर्तमान पश्चिमी चम्पारण के रहने वाले थे। मौर्य वंश में दूसरा महत्वपूर्ण नाम सम्राट अशोक का आता है जिसने 273-232 ई० पू० काल में मगध का शासन संभाला। कलिंग विजय के बाद युद्ध और बर्बरता से उसका हृदय व्यथित हो गया और जीवन का शेष भाग उसने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में लगा दिया।
मौर्य वंश के आखिरी सम्राट बृहद्रथ की
हत्या करके पुष्यमित्र ने मगध में 187 ई० पू० में शुंग वंश के राजत्व की स्थापना की। इसके बाद तो
सन् 320 तक, जब तक कि चन्द्र गुप्त ने गुप्त
साम्राज्य की जड़ें पाटलिपुत्र में नहीं जमा दीं, यूनानियों, शकों, कुषाणों आदि ने मगध पर शासन किया। गुप्त
वंश के राजाओं चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य आदि ने एक बार फिर मगध को उसका
पुराना गौरव वापस दिलवाया। परन्तु पाँचवीं सदी के अन्त में हूणों के आक्रमण ने एक
बार फिर मगध की समृद्धि में सेंध लगाई और हूणों से लुका छिपी सातवीं शताब्दी के
मध्य तक चलती रही जबकि पाटलिपुत्र पर सन् 641 में हर्षवर्द्धन का कब्जा हुआ पर यह
स्थायी नहीं हो पाया और गुप्तवंश किसी तरह घिसट-घिसट कर आठवीं शताब्दी तक शासन में
बना रहा और गुप्तवंश के बाद बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक पाल वंश का शासन
पाटलिपुत्र पर रहा। इन्द्रद्युम्न इस वंश का आखिरी राजा था। उसी के काल में मगध पर
बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ।
बिहार का कोई भी चर्चा नालन्दा और
विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की बात किये बिना पूरा नहीं होता। चीनी यात्री फाहियान
ने, जो कि भारत में सन् 405-411 के बीच रहा था, नालन्दा के बौद्ध विहार का वर्णन तो अपने
लेखों में किया है पर विश्वविद्यालय के बारे में खामोश है। परन्तु हुएनसांग (भारत
में निवास सन् 630-643 ई०) ने अवश्य ही नालन्दा के शैक्षणिक
वैभव की बहुत प्रशंसा की है। इस विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न शैक्षणिक वैभव
की बहुत प्रशंसा की है। इस विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न कोनों तथा विदेशों से
आये लगभग दस हजार छात्र वहाँ रहकर शिक्षा पाते थे। वहाँ व्याकरण, विधि, साहित्य, दर्शन आदि बहुत से विषयों की पढ़ाई होती
थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये किसी भी विद्यार्थी को द्वार पण्डित देना
पड़ता था और उसके सन्तुष्ट होने पर ही विद्यार्थी प्रवेश पा सकता था। इस
विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजाओं ने पाँचवीं शताब्दी में की और इसे
राज्याश्रय में रखा। किंवदन्तियों के अनुसार नालन्दा विश्वविद्यालय का निर्माण
सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने करवाया था परन्तु इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं मिलते।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल
वंशीय राजाओं ने आठवीं शताब्दी में वर्तमान भागलपुर के दक्षिण-पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर दूर पाथरघाट पहाड़ों में की थी।
इस विश्वविद्यालय के एक प्रधान आचार्य अतीश श्रीज्ञान दीपंकर बहुत प्रसिद्ध हुये
थे जिन्हें तिब्बत के राजा ने ग्यारहवीं शताब्दी में धर्म प्रचार के लिये तिब्बत
बुलाया था। इस विश्वविद्यालय में 108 प्राध्यापक कार्यरत थे और इसके सभा भवन में 8,000 व्यक्ति एक साथ बैठ कर धर्म चर्चा सुन
सकते थे। यहाँ वेद, वेदान्त, सांख्ययोग, मीमांसा, बौद्ध दर्शन आदि विषयों की शिक्षा दी
जाती थी। परन्तु जब तिब्बत के भिक्षु तीर्थ यात्री धर्मस्वामी सन् 1206 में इस क्षेत्र में आये थे तब उन्हें इस
विश्वविद्यालय के केवल भग्नावशेष देखने को मिले।
इन दोनों विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त
उदान्तपुरी विहार (वर्तमान बिहार शरीफ) नालन्दा के पास ही अवस्थित था। इस विहार की
स्थापना नवीं शताब्दी में पाल वंशीय राजाओं ने की थी पर यह कभी भी नालन्दा या
विक्रमशिला का मुकाबला नहीं कर पाया।
इसी तरह आठवीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य
और मण्डन मिश्र के बीच महिषी (वर्तमान सहरसा) में शास्त्रार्थ हुआ था। जिसकी मध्यस्थता
मण्डन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती ने की थी। मण्डन मिश्र तो यह शास्त्रार्थ हार
गये थे पर भारती ने शंकराचार्य से स्वयं शास्त्रार्थ करके उन्हें अतिरिक्त अध्ययन
के लिये समय माँगने पर मजबूर कर दिया था। वैसे इस बात पर विवाद है कि यह महिषी वही
महिष्मती है जहाँ शंकराचार्य और मण्डन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था।
विद्वानों की परम्परा में मिथिला के
भानुदत्त मिश्र, रत्नेश्वर, ज्योतीश्वर, भगदत्त, पृथिवीधर आचार्य, गंगेश्वर उपाध्याय, जगद्धर, विद्यापति, शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र तथा प्रभाकर मिश्र आदि
अग्रगण्य हैं। विद्यापति न केवल मिथिला के घर-घर में रचे बसे हैं, उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दी और बांग्ला
साहित्य को दिशा देने का भी काम किया है। मिथिला की विदुषी महिलायें किसी भी मायने
में पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। ऋषि पलियों मैत्रेयी और गार्गी के अतिरिक्त 15वीं शताब्दी में लछिमा देवी, लखिया देवी, विश्वास देवी तथा चन्द्रकला देवी आदि ने
साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया।
बारहवीं शताब्दी के अंत में बिहार पर
अफगान और तुर्को के हमले शुरू हो गये थे। बख्तियार खिलजी ने पाल वंशीय राजाओं से
उनका इलाका छीन लिया और इसके साथ ही प्रशासनिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। शासन कभी
दिल्ली, कभी आगरा तो कभी जौनपुर या कभी गौड़
(बंगाल) के सुल्तानों के हाथ पड़ता रहा पर पूरे बिहार पर उनकी पकड़ नहीं बन पाई और
उनका शासन अलग-अलग हिस्सों में चलता रहा। इस क्रम में कुतुबउद्दीन ऐबक, सुल्तान गयासुद्दीन, फिरोजशाह, सिकन्दर लोदी तक कितनी ही बादशाहतें आईं
और गईं। सिर्फ शेरशाह (1540-1545) ही एक ऐसा शासक निकला जिसने अपने साम्राज्य को कायदे से
जमाने की कोशिश की। शेरशाह पटना को उसकी पुरानी शान शौकत में वापस लाना चाहता था
और इस दिशा में उसने काम भी शुरू किया। बख्तियार खिलजी के जमाने से चली आ रही
राजधानी बिहार शरीफ को वह पटना ले आया और एक नये किले का निर्माण करवाया। उसने
अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार जोधपुर, ग्वालियर, मालवा तथा रणथम्बोर तक कर लिया तथा एक अच्छी शासन व्यवस्था
की पुनः नींव डाली। शेरशाह को ही बंगाल से पंजाब तक सड़क बनवा देने का श्रेय जाता
है परन्तु शेरशाह मुगलों की बढ़ती ताकत को सम्भाल नहीं पाया और अकबर के शासन काल
में बिहार मुगलों के हाथ चला गया। बिहार के राजाओं / जागीरदारों ने हमेशा की तरह
ऐसी बाहरी सत्ताओं को कबूल नहीं किया। सिर्फ औरंगजेब के पोते अजीम उश्शान का दौर
ही ऐसा था जिसमें अजीमाबाद (यह शहर अजीम उश्शान का बसाया हुआ था और वर्तमान पटना
सिटी को इलाका कहलाता है) की गई रौनक थोड़ी वापस आई और पटना तथा बंगाल का व्यापार
बढ़ा।
सन् 1704 में मुर्शीद कुली खाँ बंगाल का शासक बना
और सन् 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद अजीमाबाद उसके
दखल में आ गया। सन् 1740 में अलीवर्दी
खाँ ने मुर्शिदाबाद में हुकूमत संभाली और इस क्रम में शासन की बागडोर जायरुद्दीन
अहमद और सिराजुद्दौला के हाथों गई जिसे अंग्रेजों ने मरवा दिया। उसके बाद मीर जाफर
और मीर कासिम अली हुकमरान बने। इनके भी जाते देर नहीं लगी और अंग्रेजों ने 1765 में अपने साम्राज्य की जड़ें मजबूत कर
लीं।
आराम से बिहार में न तो अफगान, तुर्क या मुगल शासक रह पाये और न ही
अंग्रेजों को रहने दिया गया। सन् 1857 में जगदीशपुर के बाबू कुँवर सिंह और बाबू अमर सिंह ने अंग्रेजों
को नाकों चने चबवाये। इस क्रम में एक बार बाबू कुँवर सिंह को आजमगढ़ भाग जाना पड़ा
था पर वह बहादुर फिर लौटा और अप्रैल 1858 में इसने गुलामी के बदले मौत कबूलना बेहतर समझा। बाद में
बाबू अमर सिंह भी काम आये। उधर दक्षिण बिहार में ब्रितानी, हुकूमत के खिलाफ संथाल परगना के सिद्ध, कान्हू, चाँद और भैरब बन्धुओं ने 1855-57 के बीच बगावत का परचम बुलन्द किया तो
छोटानागपुर के जंगलों में 1895-1900 के बीच विक्षोभ की आग को बिरसा भगवान ने सुलगाये रखा।
इन्हीं बाँकुरों के साथ तिलका माँझी का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है।
सन् 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने
मुजफ्फरपुर में बंगाल के दुर्नाम कलक्टर किंग्सफोर्ड से फुर्सत पाने के लिये बम
फेंका। कलक्टर तो बच गया पर प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के पहले खुदकशी कर ली और
किशोर खुदी राम बोस को फाँसी लगी।
अप्रैल 1917 में चम्पारण के एक किसान श्री राजकुमार
शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गाँधी चम्पारण आये और निलहे गोरों के उत्पीड़न के
विरुद्ध पहली बार संगठित रूप से आवाज उठी। बाद के स्वतंत्रता आन्दोलन में बहुत से
स्वनामधन्य नेता बिहार में उभरे। सर्व श्री ब्रज किशोर प्रसाद, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, वैद्यनाथ झा, जयप्रकाश नारायण तथा बाबू जगजीवन राम आदि
इसी श्रृंखला की कड़ी थे। बहुत-से विद्वानों / स्वतंत्रता सेनानियों ने बिहार को
अपनी कर्म भूमि बनाया जिनमें आचार्य कृपलानी, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, श्री काशी प्रसाद जायसवाल तथा स्वामी
सहजानन्द सरस्वती के नाम उल्लेखनीय हैं।
जहाँ बिहार में एक ओर विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिये अकुलाहट थी वहीं साहित्य की सरस धारा बहाने वाले कृतिवीर भी इस धरती पर समयसमय पर जन्म लेते रहे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री फणीश्वर नाथ 'रेणु', राष्ट्र कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' तथा नागार्जुन और शाद अजीमाबादी की कृतियों में देश की मिट्टी और चिन्तन की सोंधी गन्ध मिली हुई है। बिहार (पटना) को श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की जन्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है।

अंग्रेजों के प्रादुर्भाव के समय से प्रशासनिक रूप से बिहार कलकत्ता से शासित होता चला आया था। सन् 1857 के विद्रोह के समय से ही बिहार को एक अलग प्रान्त के रूप में देखने की ईच्छा यहाँ के लोगों में थी। श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, बाबू शालिग्राम सिंह तथा बाबू विशेश्वर सिंह के नेतृत्व में चले आन्दोलन के फलस्वरूप अप्रैल 1912 में बिहार तथा उड़ीसा एक अलग राज्य बना। अप्रैल 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। पचास के दशक के राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बिहार का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप उभरा है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और उत्तर में नेपाल से घिरे इस राज्य को पश्चिम से पूर्व की ओर बहती गंगा नदी दो भागों में बाँटती है।
भौगोलिक दृष्टि से बिहार को तीन भागों
में बाँटा जा सकता है-
उत्तर बिहार के गांगेय क्षेत्र
नेपाल की तराई और गंगा के उत्तरी किनारे के बीच अवस्थित बिहार के इस मैदानी क्षेत्र में बिहार के 20 जिले आते हैं। इसके अलावा भागलपुर जिले का नवगछिया अनुमण्डल उत्तर बिहार में पड़ता है। यह पूरा इलाका उत्तर बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। मैदानी क्षेत्र और नदियों से भरा-पूरा होने के कारण उत्तर बिहार कृषि की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध रहा है।

मध्य बिहार
बिहार में गंगा के दक्षिणी तट के मैदानी
इलाकों को साधारणतया मध्य बिहार कहते हैं। दुर्गावती, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु आदि नदियों से आच्छादित इस
क्षेत्र में जमीन उत्तर बिहार जैसी ही उपजाऊ है। कैमूर पर्वतमाला की पथरीली और
प्रायः नंगी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र के अच्छे खासे इलाके में फैली हुई हैं। मध्य
बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है।
छोटानागपुर क्षेत्र
बिहार में गंगा घाटी का दक्षिण पूर्वी
क्षेत्र पठारों और जंगलों से घिरा हुआ है और भारत की पूरी खनिज सम्पदा का एक तिहाई
से अधिक इन्हीं जंगलों, पहाड़ों और जमीन के अन्दर दबा पड़ा हुआ है। बराकर, दामोदर, सुवर्ण रेखा, किऊल, कोयल, औंरंगा, अमानत, कनहर, अजय और मयूराक्षी आदि नदियों का यह
क्रीड़ा क्षेत्र छोटानागपुर और संथाल परगना उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध
है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, स्टीयटाइट, चूना पत्थर, फायर क्ले, चीनी मिट्टी, काइनाइट, ताँबा, बॉक्साइट, एसबेस्टस, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, यूरेनियम आदि क्या-क्या इस क्षेत्र में
नहीं मिलता। यही वजह है कि बहुत से बड़े उद्योग इस क्षेत्र में अवस्थित हैं।
जमशेदपुर में टाटा समूह के टिस्को तथा टेल्को, बोकारो में इस्पात कारखाना, राँची में भारी अभियंत्रण निगम, मुरी (राँची) का अल्यूमिनियम कारखाना, पूर्वी सिंहभूम में हिन्दुस्तान कॉपर
कार्पोरेशन, सिंदरी का रासायनिक खाद का कारखाना, धनबाद-झरिया की कोयला खदानें, झींकपानी, जपला, खेलारी और जमशेदपुर के सीमेन्ट कारखाने
सभी इसी क्षेत्र में लगाये गये हैं।
इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन और विस्तृत
जल-संसाधन तथा अतुलनीय खनिज सम्पदा का स्वामी होने के बाबजूद बिहार राज्य आजकल देश
के अन्य राज्यों के मुकाबले विकास के सभी स्थापित मानदण्डों पर पिछड़ा हुआ है।
इसकी एक झलक तालिका 1-1 के आँकड़ों से
मिलती है।
बिहार–पिछड़ता वर्तमान
इतने प्राकृतिक संसाधन पास में होने के बावजूद बिहार यदि विपन्न है तो इसका दोष किसे दिया जाये। सदियों से परतंत्र रहते आने के कारण जन्मी कुंठा को या प्रशासनिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था को अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित होने के कारण एक बात तो अवश्य समझ में आती है कि यदि किसी प्रकार कृषि सुव्यवस्थित रह सके तो बिहार की अधिकांश जनता जमीन से जुड़ी रह सकेगी। दिक्कत यही है कि यहाँ की जमीन की मालिकाने के रिश्ते ज़रा उलटे हैं। यहाँ के 84-6 प्रतिशत जोतदारों के पास कृषि के लिये उपलब्ध कुल जमीन का मात्र 377 प्रतिशत हिस्सा हाथ आया है। इनमें से औसतन जोत का रकबा 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं है। उधर 15.4 प्रतिशत लोगों के हाथ 63.3 प्रतिशत जमीन है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अगर खेती में थोड़ा भी व्यवधान पड़ेगा तो बहुत से लोगों को रोजी-रोटी के लाले पड़ जायेंगे। बिहार की कृषि ज्यादातर या तो वर्षा के भरोसे या फिर भगवान के भरोसे है। बिहार लगभग हर साल सूखे या बाढ़ की पीड़ा झेलता है। कभी-कभी तो यह दोनों मेहमान एक साथ आ जाते हैं। कभी एक इलाके में सूखा तो दूसरे में बाढ़ और कभी-कभी तो एक ही जगह पर पहले सूखा और बाद में बाढ़ या फिर पहले बाढ़ और बाद में सूखा। इन दोनों मुसीबतों की जितनी भी शक्लें हैं सब की सब जानलेवा हैं। आम तौर पर बिहार अपनी भौगोलिक बनावट के कारण नदियों से घिरा होने की वजह से उत्तर में बाढ़ झेलता है और दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्रों में सूखे की मार बर्दाश्त करता है। मध्य बिहार में स्थितियाँ बदलती रहती हैं। पटना, आरा, रोहतास, भोजपुर, भभुआ आदि जिलों में सोन नहर के कारण कुछ खेती सम्भल जाती है पर इन जिलों में भी अक्सर बाढ़ आया करती है। मध्य बिहार के बाकी जिलों गया, जहानाबाद, नालन्दा, नवादा, गया तथा औरंगाबाद अक्सर सूखे की चपेट में आ जाते हैं।
बाढ़ और बिहार
हम अपने अध्ययन को बिहार में साल दर साल आने वाली बाढ़ तक सीमित रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ से होने वाली कुल क्षति का 22-8 प्रतिशत बिहार में होता है। जब कि देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुल क्षेत्र का मात्र 16:5 प्रतिशत ही बिहार में पड़ता है। इसका अर्थ यह होता है कि अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर बिहार अधिक नुकसान उठाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद बिहार में 1984, 1987 तथा 1993 में बड़ी बाढ़े आई हैं जिनमें 1987.वाली बाढ़ को प्रलयंकर बाढ़ माना जाता है। इस बाढ़ ने पूरे देश में बाढ़ के सन्दर्भ में बिहार का रुतबा कुछ और बुलन्द कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। पूरे देश के कुल 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 64-61 लाख हेक्टेयर बिहार में है। जो देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16 प्रतिशत है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र 173:50 लाख हेक्टेयर का यह 37 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 56:5 प्रतिशत केवल बिहार राज्य की आबादी है। यह तथ्य राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा भी स्वीकार किया गया है। उत्तर बिहार का कुल क्षेत्रफल 58:51 लाख हेक्टेयर है। इस भाग में 44:47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। इस प्रकार उत्तरी बिहार का लगभग 76 प्रतिशत भाग बाढ़ प्रभावित है।

यदि केवल साक्षरता को हम जीवन स्तर की गुणवत्ता नापने का एक मापदण्ड मानें तो उत्तर बिहार की स्थिति पूरे बिहार के सन्दर्भ में भी गई बीती है। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत बिहार से भी कम है। इसी तरह हम प्रति व्यक्ति बिजली की खपत का एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। “वर्ष 1978-79, 1980-81 और 1981-82 में सारे देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्रमशः 150-73 किलोवाट, 155:62 किलोवाट तथा 143:41 किलोवाट थी। वहीं बिहार के लिये इन्हीं वर्षों में प्रति व्यक्ति क्रमशः 87:15 कि० वा०, 82:58 कि० वा० तथा 81:13 कि० वा० की खपत हुई। यदि उत्तर बिहार को अलग करके देखा जाय तो इन वर्षों में यहाँ बिजली की खपत प्रति व्यक्ति क्रमशः 26:60 कि० वा०, 1482 कि० वा० तथा 13:43 कि० वा० थी यानी राष्ट्रीय औसत के दसवें हिस्से से भी कम बिजली उत्तर बिहार में उपलब्ध है। इसके अलावा आजकल बिहार में लगभग 9 लाख हेक्टेयर जमीन जल जमाव से ग्रस्त है और यह लगभग पूरी की पूरी उत्तर बिहार में है जिसके लिये इस इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ तथा क्षेत्र की ज़मीन की बनावट जिम्मेवार है। अत्यधिक जल जमाव से कृषि उत्पादन तथा कृषि सम्बद्ध रोज़गार, दोनों पर ही बुरा असर पड़ा है और आर्थिक विपन्नता बढ़ी है।

घाघरा, गण्डक, बूढ़ी गण्डक, बागमती, अधवारा समूह, कमला,कोसी, महानंदा प्रमुख हैं। यह सभी नदियाँ अपनी धारा परिवर्तन के लिये प्रसिद्ध रही हैं। जिनमें कोसी की धारा सबसे अधिक अस्थिर है। इस पूरे इलाके के पानी की निकासी का एक ही रास्ता गंगा से होकर है और यह नदी पूरे प्रान्त के लिये जीवन रेखा का काम करती है।

गंगा
दक्षिण बिहार की सुवर्ण रेखा घाटी को
छोड़कर बाकी पूरे बिहार के पानी की निकासी गंगा के माध्यम से होती है और इसलिये
गंगा बिहार के लिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वयं बिहार भी गंगा के लिये कम
महत्वपूर्ण नहीं है। गंगा का एक नाम जाह्नवी है। आधुनिक भागलपुर के सुलतानगंज के
पास गंगा की धारा में एक पहाड़ी पर भगवान शंकर का एक मन्दिर है। कहते हैं कि यहाँ
कभी जलु ऋषि का आश्रम हुआ करता था। भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों के उद्धार के लिये
गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक ले जाने के लिये राजी कर लिया तब गंगा उनके
पीछे-पीछे चल पड़ी और रास्ते में जो कुछ भी पड़ता था उस पर अपनी छाप छोड़ती जा रही
थी। परन्तु अब मुकाबला जट्स ऋषि से था जिनके आश्रम को गंगा बहा ले जाने वाली थी।
गंगा का प्रवाह देखकर ऋषि को क्रोध आया और वे गंगा को पी गये। बेचारे भगीरथ ने
जैसे-तैसे गंगा को मुक्त करने के लिये ऋषि को मनाया तब उन्होंने गंगा को अपने पेट
से बाहर निकाला। यहीं से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा।
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में 7,016 मीटर की ऊँचाई से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उद्गम पर इस नदी को भागीरथी कहते हैं जो कि देव प्रयाग के पास अलकनन्दा से संगम करके गंगा नाम धारण करती है और लगभग 250 कि० मी० नीचे बहने के बाद ऋषिकेश के पास मैदानों में उतरती है। इसके बाद यह नदी हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी होते हुये वाराणसी से लगभग 155 कि० मी० की दूरी पर बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में इस नदी की कुल लम्बाई लगभग 1450 कि० मी० है। जिसमें गंगोत्री से लेकर देव प्रयाग तक की भागीरथी की लम्बाई शामिल है। बिहार में इस नदी की लम्बाई लगभग 438 कि० मी० है जिसमें से 110 कि० मी० दूरी में यह नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा बनाती हुई बहती है।

राजमहल के पास बिहार से निकलने के बाद गंगा फरक्का से 40 कि० मी० पूर्व की ओर बढ़कर दो भागों में बँट जाती है और इन दोनों धाराओं के नाम अलग-अलग हो जाते हैं। बायीं धारा जो पूर्व की ओर जाती है पद्मा कहलाती है और भागीरथी नाम की दायीं धारा दक्षिण की ओर बहते हुये मुर्शिदाबाद, बर्द्धमान, चौबीस परगना, कलकत्ता होते हुये कई धाराओं में बँटती हुई सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की कुल लम्बाई 520 कि० मी० है।

जहाँ इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा नदियाँ हों वहाँ बाढ़ का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। वस्तुतः इस इलाके की बनावट ही ऐसी है कि इसमें बाढ़ आना और नदियों का धारा परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
उत्तर बिहार में पश्चिम चम्पारण में सोमेश्वर पहाड़ों के सबसे ऊँचे इलाके र ३ टेहर के सबसे निचले इलाके 170 मीटर से 40 मीटर कन्टूर लाइनों के बीच अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में जमीन और नदियों का ढाल कम होने के कारण वर्षा का पानी आसानी से निकल नहीं पाता और बड़े इलाके पर फैलता है। गंगा का स्तर अधिक होने पर उसकी सहायक नदियों का पानी भी ठहर जाता है पानी के फैलाव से खेतों पर जहाँ एक ओर नई मिट्टी पड़ जाया करती है और जमीन की उर्वरा शक्ति फिर तरो ताजा हो जाती है वहीं बाढ़ से, कुछ समय के लिये ही सही, जीवन शैली अस्त-व्यस्त हो जाया करती है। कभी-कभी अगर भयंकर बाढ़ आ गई तो फसल के साथसाथ जान माल का काफी नुकसान हो जाया करता है।

उत्तर
बिहार की बाढ़ की इस समस्या को समझने के लिये हमें गंगा घाटी के निर्माण की
प्रक्रिया को जान लेना रुचिकर होगा और इसके साथ ही जरूरी होगा कि वर्षा और पानी की
विभिन्न स्थितियों को, जिसे
जलीय चक्र कहते हैं, थोड़ा
समझ लिया जाय और तब वह जानना बहुत आसान हो जायेगा कि नदियाँ अपनी धारायें कैसे
बदलती हैं और बाढ़ का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होने लगेगा।
गंगा घाटी का निर्माण
आज से लगभग 33,500 लाख
वर्ष पहले हमारी पृथ्वी सूर्य से एक आग के गोले की शक्ल में अलग हुई। तब इसकी ऊपरी
सतह पर पिघलती चट्टानों की परत हुआ करती थी। समय के साथ भारी चट्टानें तो पृथ्वी
। के गर्भ में समाती गई पर हलकी चट्टानें ऊपर रह गईं। इन्हीं गली हुई चट्टानों पर
भूकम्पों के असर तथा उसकी वजह से निकली हुई गैसों से वातावरण का निर्माण हुआ।
धीरे-धीरे जब पृथ्वी और ज्यादा ठण्डी हुई तब वातावरण में भाप की शक्ल में मौजूद
पानी ठण्डा होकर वर्षा की बून्दों में बदला और जमीन पर वापस गिरा और लाखों साल ऐसा
होते रहने के कारण समुद्रों का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी की सतह पर तापक्रम में
गिरावट आई मगर जमीन के अन्दर की गर्मी और उथल-पुथल जारी रही और यह आज भी जारी है।
आज
हमारी पृथ्वी की सतह (पपड़ी), कई
बड़े-बड़े मजबूत टुकड़ों में बटी हुई है और इन टुकड़ों पर बहुत से देश और यहाँ तक
कि महाद्वीप तक आबाद हैं। मगर आज से लगभग 30 करोड़
साल पहले तक पृथ्वी की सतह का इस तरह के टुकड़ों में विभाजन नहीं हुआ था। उस समय
तक सारे द्वीप या महाद्वीप एक ही भूखण्ड के रूप में मौजूद थे। परन्तु पिछले बीस
करोड़ वर्षों में न सिर्फ पृथ्वी की सतह में दरारें पड़ी हैं बल्कि इसके कारण बटे
हुए टुकड़ों में, जिन्हें
प्लेट कहते हैं, गति भी आई है। इन प्लेटों
के फैलाव से हमारी आज की दुनियाँ का जो स्वरूप उभरा है वह हमारे सामने है।
यह सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। आज भी यह प्लेटें आपस में एक-दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं। इनका एक हिस्सा एक दूसरे पर चढ़ जाता है, आदि-आदि कितने ही काम हमारी धरती के नीचे हर लमहे में हो रहे हैं जिनका कभी-कभी हम लोगों को भूकम्प की शक्ल में अन्दाजा लगता है। एक अनुमान के अनुसार दुनियाँ में हर साल लगभग 10,000 छोटे-बड़े भूकम्प दर्ज किये जाते हैं मगर उनमें से जान-माल को नुकसान पहुँचाने वाले भूकम्पों की तादाद दस से ज्यादा नहीं होती।

बीसवीं
शताब्दी के शुरुआती दौर में अमेरिका के वैज्ञानिक टेलर तथा जर्मनी के वैज्ञानिक
अल्फ्रेड ने पृथ्वी के विकास तथा महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया था। इन दोनों के अध्ययन तथा बाद में हुये शोधों से पृथ्वी के विकास की जो तस्वीर
सामने आती है उससे जाहिर होता है कि एक समय दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी सीमा तथा
अफ्रीका की पश्चिमी सीमा रेखा एक ही थी। इसी तरह पश्चिमोत्तर अफ्रीका की सीमा
उत्तरी अमेरिका से मेल खाती थी। आज का ऑस्ट्रेलिया कभी अंटार्कटिका का हिस्सा था।
आज के भारत का विन्ध्य और राजमहल पर्वत मालाओं के नीचे का हिस्सा कभी दक्षिणी
ध्रुव के बीच एक द्वीप की तरह हँसा हुआ पड़ा था। जमीन के इस टुकड़े को
भू-वैज्ञानिक गोण्डवाना लैण्ड कहते हैं। समय के साथ-साथ गोण्डवाना लैण्ड
पूर्वोत्तर दिशा में एशिया के नजदीक आने लगा। टेथीज़ सागर नाम का एक समुद्र एशिया
और गोण्डवाना लैंण्ड के बीच में था। मगर आज से लगभग पाँच करोड़ तीस लाख साल पहले
गोण्डवाना लैण्ड और एशिया मुख्य भूमि एक-दूसरे से जुड़ गये। टेथीज़ सागर पहले तो
धीरे-धीरे सँकरा हुआ पर बाद में एशियाई मुख्य भूमि पर होने वाली लगातार बारिश और
उसके साथ आने वाली बालू और सिल्ट ने इस समुद्र को पूरा ही पाट दिया।
एशिया मुख्य भूमि और
गोण्डवाना लैण्ड के बीच का पटा हुआ समुद्र ही आज
की गंगा घाटी है।
इस
पूरे किस्से का एक दिलचस्प पहलू और भी है। वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि जब
एशिया और गोण्डवाना लैण्ड का जुड़ाव हुआ तो सबसे पहले आज की छोटानागपुर-संथाल
परगना की राजमहल पर्वतमाला तथा उत्तर पूर्वी राज्यों की गारो पर्वतमाला एक-दूसरे
से टकराईं। इस संयोग से पानी के बहाव के लिये पूर्व का रास्ता बंद हो गया। अब जो
भी पानी एशियाई भूमि के दक्षिण या गोण्डवाना लैण्ड के उत्तर में बरसता था वह सब का
सब पश्चिम की ओर बहता हुआ समुद्र में पहुँचता था। यानी उस समय गंगा सचमुच उल्टी
बहती थी जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी का पानी भी इस नदी से होकर अरब सागर में जाकर मिलता
था। परन्तु धीरे-धीरे पूरा गोण्डवाना लैण्ड एशिया से जुड़ा, उसका
पश्चिम-उत्तर वाला भाग ज्यादा मजबूती से एशिया की ओर बढ़ा और गारो तथा राजमहल
पहाड़ियाँ फिर एक दूसरे से अलग
हुईं। इस तरह ज़्यादातर पानी की निकासी पूर्व की ओर होने लगी और गंगा का जन्म हुआ
जो कि हिमालय से निकल कर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा तय करती है।
गोण्डवाना
लैण्ड की उत्तरी सीमा पर जो पहाड़ या चट्टानें थीं, जिन्हें राजमहल श्रृंखला और
विन्ध्य पर्वत माला कहते हैं, वह तो
काफी पुरानी थीं मगर एशियाई जमीन महज़ कच्ची और भुर-भुरी मिट्टी थी। ऐसी भुरभुरी
मिट्टी पर जब गोण्डवाना लैण्ड का दबाव पड़ा तो वह पहाड़ों में तबदील हुई पर यह
पहाड़ पथरीले न होकर अभी तक कच्ची मिट्टी के हैं जिनके पथरीले बनने में लाखों
वर्षों का समय लगेगा। आज के नेपाल और भूटान के
पहाड़ अभी नवजात हैं और इसी तरह की मिट्टी के ढेर हैं। ऐसे में जब इन पहाड़ों पर
पानी बरसता है तो उनसे निकलने वाली नदियों में पानी के साथ-साथ मिट्टी और बालू की
एक अच्छी खासी मात्रा चली आती है। गंगा के उत्तर के पहाड़ों से सदियों से बहकर आने
वाली मिट्टी तथा बालू से ही गंगा घाटी और उसके मैदानों का निर्माण हुआ।
चित्र-17 में
पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों को दिखाया गया है तथा चित्र16 में इन
प्लेटों की वर्तमान गति की दिशा भी दिखाई गई है। इन चित्रों से दो
बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि आज की भारत भूमि का दबाव उत्तर की ओर एशियाई
मुख्य भूमि पर बना हुआ है और दूसरी बात यह कि भारत के लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भाग
में दो प्लेटों का संधि क्षेत्र है। प्लेटों के आपसी टकराव या रगड़ के कारण इस
क्षेत्र में भीषण भूकम्प आते रहते हैं।
पृथ्वी
के भूमि खण्डों का विस्थापन एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जिसको सौ-पचास वर्षों
के अन्तराल पर अनुभव नहीं किया जा सकता है। इस तरह के परिवर्तन हजारों साल के
फासले पर ही महसूस किये जा सकते हैं। गंगा घाटी का निर्माण भी इसी तरह का एक वाकया
है। हजारों लाखों वर्षों से हो रही बारिश और उसकी वज़ह से आई सिल्ट बालू
ने इस घाटी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है।
जलीय चक्र
बारिश के अपने उसूल हैं। मोटे तौर पर सूर्य की धूप के कारण समुद्र का पानी भाप बन कर ऊपर आसमान की ओर उठता रहता है। ऊपर पहुँचने पर तापक्रम कम होने के कारण यह भाप ठण्डी होकर बादल की शक्ल अख्तियार करती है और हवा के असर से जमीन की ओर का रुख करती है। बादलों में यह पानी वर्षा की बून्द, ओले या बर्फ की शक्ल में जमा रहता है और अनुकूल परिस्थितियों में जमीन पर गिरता है तथा प्राणियों के लिये जीवन का आधार बनता है। ओस या कोहरा भी इसी पानी का दूसरा रूप है। जमीन पर गिरने वाले पानी का कुछ हिस्सा नालों-नदियों की मदद से वापस समुद्र में पहुँच जाता है। कुछ पानी पेड़ पौधों के श्वासोच्छवास आदि क्रियाओं से वातावरण में वापस पहुँच जाता है और कुछ पानी जमीन के अन्दर जाकर भूमिगत जल की तह को समृद्ध करता है। वास्तव में जमीन के नीचे भी पानी की लगभग वैसी ही धारा मौजूद रहती है जैसा कि नदियों आदि की शक्ल में हम जमीन के ऊपर देखते हैं। जमीन के नीचे का पानी भी सतही पानी की तरह समुद्र से अपना सम्पर्क साध लेता है। इस प्रकार समुद्र से समुद्र तक का पानी का चक्र पूरा हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जलीय चक्र (Water Cycle) कहते हैं जिसमें प्रकृति समुद्र के खारे जल को उपयोगी मीठे जल में परिवर्तित करती है। पृथ्वी पर मीठे पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चित्र में जलीय चक्र की विभिन्न दशाओं को दिखाया गया है। समुद्र से समुद्र तक लगातार चलने वाले पानी का यह सफर कभी नहीं रुकता है।

नदियों का धारा परिवर्तन
पहाड़ी
इलाकों में ज़मीन का ढाल इतना ज्यादा होता है कि पानी रुक नहीं पाता मगर जैसे ही
नदियाँ पहाड़ों से मैदानी इलाकों में उतरती हैं ज़मीन का ढाल बहुत कम हो जाता है
जिसकी वज़ह से पानी की रफ्तार पहले। के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है। पहाड़ों से
उतरता हुआ नदी का पानी सिर्फ़ पानी ही नहीं होता, इसके
साथ एक अच्छी खासी मात्रा में पेड़-पौधे, चट्टानें, पत्थर, बालू
और मिट्टी होती है। पत्थर, चट्टानें
वगैरह तो ज़मीन का ढाल कम होने पर बहुत आगे तक साथ नहीं चल पाते पर मिट्टी/रेत तो
नदी के पानी के साथ चलती ही रहती है। ज़मीन का ढाल और पानी की रफ्तार कम होने की
वजह से इस मिट्टी/रेत को नदी की पेटी में बैठने का मौका मिलता है। इसके अलावा नदी
जब अपने किनारे तोड़ कर बहती है तो पानी के साथ आई बालू और मिट्टी को पूरे इलाके
पर फैलने और जमा होने का मौका मिलता है। नदियाँ इसी तरीके से ज़मीन का निर्माण
करती हैं।
नदियों की रफ्तार में कमी उनके पहाड़ों से मैदान में उतरने की जगह दिखाई पड़ती है मगर जहाँ यह नदियाँ किसी बड़ी नदी से मिलती हैं वहाँ बाढ़ के समय अक्सर छोटी नदी की रफ्तार ठहराव में बदल जाती है क्योंकि बड़ी नदी में पानी के लेवेल के मुताबिक ही छोटी नदी का पानी बह कर निकल पाता है। करीब-करीब ऐसी ही स्थिति समुद्र के किनारे समुद्र में उठते ज्वार तथा वहाँ समुद्र में मिलने वाली नदी के मुहाने पर पैदा होती है। रफ्तार में ठहराव के कारण इन दोनों जगहों पर मिट्टी / रेत का जमाव तेज होता है जिससे नई-नई ज़मीन या डेल्टा का निर्माण होता है।

अमेरिका
की मिस्सीसिपी नदी के मुहाने पर 6.5 कि०
मी० चौड़ी पट्टी का निर्माण सौ वर्षों के अन्दर हो जाया करता है। चीन की
यांग्टीसी-कियांग नदी में ऐतिहासिक काल से अब तक 48 कि०
मी० चौड़े डेल्टा का निर्माण हुआ है जबकि चीन का शोक' ह्यांग
हो नदी ने ईसा पूर्व 5,500 से
लेकर आधुनिक काल तक लगभग 500 कि०
मी० चौड़े डेल्टा का निर्माण किया है। इसी तरह गंगा नदी ने भी समुद्र से लगभग 250 कि०मी०
पहले तक के इलाके पर डेल्टा का निर्माण किया हुआ है।
यूरोप के ज्यादातर देशों के एक बड़े हिस्से में बारिश करीबन पूरे साल होती रहती है। हमारे देश में बरसात का मौसम होता है और पूरे साल बरसने वाले पानी का लगभग 87 फीसदी पानी मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच में बरस जाता है। बारिश और बाढ़ खत्म होने के साथ-साथ जो कुछ भी रेत /मिट्टी इलाके पर जमा होनी होती है, हो चुकती है। बाढ़ की वज़ह से कहीं मोटी रेत/मिट्टी की परत जमा होती हैं तो कहीं पतली कहीं कटाव के कारण गड्ढे बनते हैं तो कहीं जल जमाव हो जाता है। आने वाले मौसम में जब बाढ़ का पानी फिर चढ़ता है तो पिछले साल की जमा मिट्टी को काट कर नया रास्ता बना लेता है। कभी-कभी यह नये रास्ते इतने ज्यादा बड़े और कारगर होते हैं कि नदी की धारा ही इस नये रास्ते पर फूट पड़ती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जिन नदियों के पानी में रेत / मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी उनके कछार में रेत /मिट्टी का जमाव भी ज्यादा होगा और ऐसी नदियों की धारा में बदलाव की गुंजाइश भी ज्यादा होगी। यही कारण है कि गंगा में उसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों में धारा के बदलाव की सम्भावनायें गंगा के बायें किनारे पर मिलने वाली नदियों के मुकाबले कम है क्योंकि दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ पठारी इलाकों से आकर गंगा में मिलती हैं जबकि गंगा के उत्तरी या बायें किनारे पर आकर मिलने वाली नदियाँ हिमालय जैसे कच्चे और भुरभुरे पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। और अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी/ रेत लेकर आती हैं। ज्यादा गाद वाली नदी की धारा बदलना भी उतनी ही प्राकृतिक और स्वाभाविक घटना है। जितना कि पृथिवी की विभिन्न प्लेटों में गति, पानी बरसना और नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण।

इस तरह
बाढ़, कटाव, जल-जमाव, नदियों
के धारा परिवर्तन जैसे सवाल गंगा के उत्तरी छोर पर ज्यादा गंभीर हैं। यह सवाल उन
जगहों पर और भी ज्यादा गंभीर हैं जहाँ जमीन का ढाल लगभग सपाट है। गंगा घाटी में
ऐसी जगहें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर
बिहार के मैदान और उत्तर बंगाल में पाई जाती हैं। मगर इसका मतलब यह कतई नहीं हैं
कि गंगा के दाहिने किनारे पर बाढ़ के लिहाज से पूरा अमन चैन है। परेशानियाँ वहाँ
भी, कम से कम मैदानी इलाकों
में, उतनी ही हैं जितनी कि
गंगा के उत्तरी किनारे पर और बिहार के भोजपुर, रोहतास, पटना, मुंगेर, भागलपुर
और साहेब गंज जिलों में बाढ़ से पैदा होने वाले मसले इसका उदाहरण हैं। इस घाटी के
दक्षिण में विन्ध्य तथा सतपुड़ा पर्वत मालायें हैं जो कि गोण्डवाना लैण्ड का
हिस्सा हैं। यह पहाड़ियाँ हिमालय के पहाड़ों से कहीं ज्यादा पुरानी हैं। और मजबूत
पत्थर हो चुकी हैं। इस वजह से इन पहाड़ियों पर शिवालिक और हिमालय जितना भू-क्षरण
नहीं होता। परन्तु क्षेत्रफल के लिहाज से गंगा के उत्तर वाला इलाका बाढ़ से ज़रा
ज्यादा परेशान रहता है।
बाढ़े और उनका ऐतिहासिक संदर्भ
गंगा घाटी के निर्माण की
प्रक्रिया, पानी का समुद्र से समुद्र
तक का सफर तथा नदियों के धारा परिवर्तन का कारण समझ लेने के बाद एक चीज़ जो स्पष्ट
होकर सामने आती है वह यह है कि न तो पृथ्वी के भूखण्डों के विस्थापन रुकने की कोई
उम्मीद है और न ही समुद्र से समुद्र तक का पानी का सफर थमेगा । बारिश होती ही
रहेगी और कच्ची भुरभुरी मिट्टी पर जब यह पानी पड़ेगा तो भूक्षरण होगा, नदियाँ
अपनी धारायें बदलेंगी और बाढ़ आती रहेगी। मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से इस पूरे
क्रिया कलाप में भू-क्षरण, नदियों
के धारा परिवर्तन तथा बाढ़ों से मुकाबला करने के क्षेत्र में थोड़ा बहुत बदलाव ला
सकता है। इससे ज्यादा उसकी औकात अभी तक नहीं बनी है।
यहाँ
एक बात ध्यान देने लायक है कि उत्तर बिहार, या यूँ
कहा जाय कि गंगा घाटी का पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र, बहुत
ही उपजाऊ इलाका है। जिसकी उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बाढ़ के समय नदियों के पानी
के साथ आई सिल्ट के कारण निखरी है। आदिकाल से कृषि समृद्ध क्षेत्र होने के कारण
विभिन्न सभ्यताओं का विकास इस इलाके में हुआ ।
प्रकृति
लेकिन खैरात नहीं बाँटती। उसने अगर गुलाब बनाये हैं तो उसके साथ काँटों का इन्तजाम
भी कर रखा है। वर्षा के रूप में जहाँ-जहाँ भी मीठे पानी का समृद्ध स्रोत है और
थोड़ी-थोड़ी दूरी पर नदियों का जाल बिछा हुआ है वहीं-वहीं पर बाढ़, कटाव
तथा नदियों के धारा परिवर्तन आदि की बातें भी ज्यादा सुनने को मिलती हैं। नदियाँ
अपने उद्गम से लेकर समुद्र तक के अपने रास्ते में बाढ़ के समय मिट्टी / बालू को एक
बड़े क्षेत्र पर फैलाने तथा समुद्र तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम हैं। वास्तव
में इस प्रकार भूमि निर्माण करना नदियों का स्वाभाविक गुण है।
गंगा
घाटी का यह क्षेत्र निश्चय ही एक समय समुद्री बालू और खारे पानी का इलाका रहा
होगा। मगर बारिश की वजह से उत्तर में हिमालय की कच्ची मिट्टी बहकर नीचे आना शुरू
हुई जिससे जमीन उपजाऊ बनना शुरू हुई।
जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस जगह की जमीन की गिनती दुनियाँ के सबसे उपजाऊ जमीन के साथ की जाती है और यही नदी को भी केवल जल संसाधन (Water Resources) का स्रोत माना है। भौतिकवादी मान्यताओं से हटकर हमारे लिये नदियों का महत्व एक जीवनदायी शक्ति का रहा है। नदियाँ भारत की संस्कृति का आधार रही हैं। आदिकाल से ही कितनी सभ्यतायें इन नदियों के किनारे विकसित हुईं और कालक्रम में प्रकृति के गर्भ में समा गईं परन्तु हमारा इन नदियों से सम्बन्ध हमेशा ही निश्छल और वत्सला मातृशक्ति और उसके उपासकों का रहा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में नदियों को ‘विश्वस्य मातरः' अर्थात् लोकमाताये कह कर जहाँ उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है वहीं कौटिल्य जैसे विद्वानों ने ऐसे स्थानों को निवास के लिये ही वर्जित माना है, जहाँ कोई सजला नदी निरन्तर बहती न हो। 'न तत्र दिवसम् वसेत्’-ऐसी जगह पर एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिये-ऐसा कह कर उन्होंने नदियों के महत्व को रेखांकित किया था। अपने सभी मांगलिक अनुष्ठानों में भारतीय कभी भी देवताओं तथा पूर्वजों के आवाहन के साथ साथ नदियों का आवाहन करना नहीं भूलते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु तथा कावेरी का स्मरण किये बिना हमारा कोई भी शुभ कर्म पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। पवित्रता की मिसाल देने के लिये हम लोग नर्मदा को याद करते हैं और गंगा की सन्तान कहलाने में हम लोगों का कद थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ‘मरने पर गंगा मिलै’ की ईच्छा केवल कबीर जैसे साधकों में शायद इस लिये नहीं जन्मी कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गंगा के किनारे बिता दिया था। भाव वश किसी भी नदी को गंगा कहने की परम्परा हमारे जन मानस में आज भी जीवित है। ‘कालिन्दि कूल कदम्ब की डारन' कहे बिना भगवान कृष्ण की चर्चा अधूरी रह जाती है तो भगवान राम को सरयू के सामने कितनी ही बार वाल्मीकि ने नतमस्तक होते देखा है। क्षिप्रा ने कालिदास की लेखनी को लालित्य प्रदान किया। तीर्थों की कल्पना (तीर्थ का शाब्दिक अर्थ नदी का घाट होता है) ने नदियों के प्रताप की स्वीकृति को अभिव्यक्ति दी है। ऐसे विशिष्ट अवसरों पर नदी स्नान की हमारी अलग परम्परा रही है। गंगा दशहरा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, संक्रान्ति आदि कितने ही ऐसे अवसर हैं जब कि नदी निरपेक्ष लोगों को नदी के पास लाने की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने कर दी थी। नदियों की पवित्रता बनाये रखने के लिये उत्सर्जन आदि के विरुद्ध शास्त्रों में कड़े दिशा निर्देश थे। बिहार का छठ पर्व सूर्य उपासना के साथ-साथ नदियों के प्रति हमारी श्रद्धा का अप्रतिम उदाहरण है।

हमारी इसी समृद्ध धरोहर की एक छोटी सी कड़ी उत्तर बिहार के पूर्वी जिलों, किशनगंज, पूर्णियाँ और कटिहार से होकर बहने वाली महानन्दा नदी है। महाभारत में कौशिकी (कोसी) नदी के पास बहने वाली दो नदियों, नन्दा तथा अपर नन्दा का जिक्र आया है जहाँ पाण्डव अपने अज्ञातवास के क्रम में आये थे। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल की अपर नन्दा ही वर्तमान महानन्दा है। महानन्दा की एक सहायक धारा कनकई का वर्णन भी महाभारत में आया है जहाँ उसे कनकनन्दा कहा गया है। महानन्दा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिये प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन कटिहार जिले में दुर्गापुर और कल्याणी में मेला लगता है। इसी दिन इस क्षेत्र में काढ़ा गोला के पास गंगा के किनारे भी मेला लगता है।

महानन्दा नदी
महानन्दा
उत्तर बिहार की एक मुख्य नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले
में करसियांग के 6 कि०मी०
उत्तर में हिमालय पर्वत माला में चिमले के पास है जहाँ से यह नदी 2062 मी० की
ऊँचाई से गंगा तक की अपनी 376 कि०
मी० लम्बी यात्रा शुरू करती है। इस नदी के प्रवाह पथ को चित्र 1:11 में
दिखाया गया है। कनकई से संगम के बाद महानन्दा बरही-गुआहाटी राष्ट्रीय मार्ग 31 (नेशनल
हाइवे 31) को बाघझोर के पास पार
करते हुये बागडोब तक आती है जहाँ इसकी धारा दो भागों में बँट जाती है। बागडोब में
लगभग दक्षिण की ओर सीधी बहने वाली धारा को झौआ शाखा कहते हैं और महानन्दा का
अधिकांश जलप्रवाह आजकल इसी धारा से होकर गुजरता है। झौआ शाखा में ही आगे चलकर
दाहिने तट पर पनार नदी आकर मिलती है। यह शाखा आगे चलकर कटिहार बारसोई रेल लाइन को
झौआ के पास तथा कटिहार-मालदा रेल लाइन को लाभा के पास पार करती है। महानन्दा की
झौआ शाखा से एक अन्य सहायक नदी घसिया, लाभा
के नीचे आकर मिलती है। यहाँ से महानन्दा की झौआ शाखा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले
में प्रवेश कर जाती है और सुरमारा के पास गंगा नदी से संगम करती है। बागडोब
पर महानन्दा की दूसरी शाखा, जो कि
दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, कटिहार-बारसोई
रेल लाइन को बारसोई के पास पार करती है। बारसोई के नीचे यह धारा भी दो भागों में
बंट जाती है। इनमें से पूर्व की ओर बहने वाली धारा ज्यादा सक्रिय है जबकि पश्चिम
की ओर जाने वाली धारा छिछली हो गई है और उसमें सिल्ट-बालू का जमाव हो गया है। यह
धारा पुनः सुबर्नपुर के निकट मुख्य धारा में मिल जाती है। अब यह संयुक्त धारा
बांग्लादेश में गोदागिरी घाट के निकट गंगा में मिल जाती है।
महानन्दा
का कुल जलग्रहण क्षेत्र 24753 वर्ग
कि०मी० है जिसमें से 5293 वर्ग
कि०मी० नेपाल में, 6677 वर्ग
कि०मी० पश्चिम बंगाल में, 7957 वर्ग
कि०मी० बिहार में तथा बाकी बांग्लादेश में पड़ता है। डेंगरा घाट के उत्तर में इस
नदी के तल का ढलान अपेक्षाकृत अधिक है जो कि ढंगरा घाट के नीचे क्रमशः कम होता
जाता है जिसके कारण नदी की प्रवाह क्षमता धीरे-धीरे घटती जाती है और नदी अपने
किनारों को लाँघ कर अक्सर छलक जाया करती थी। निचले हिस्सों में झौआ शाखा के तल का
ढलान 0.099 मी०/कि०मी० तक है जबकि
बारसोई शाखा के तल का ढलान 0.146 मी०/प्रति
कि०मी० है। साठ के दशक और उसके बाद की सरकारी रिपोर्टों के अनुसार ढलान की इस कमी
के कारण महानन्दा के निचले हिस्सों में लम्बे समय तक (लगभग एक सप्ताह तक) जल-जमाव
की स्थिति बनी रहा करती थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन पूर्णियाँ का दक्षिणी हिस्सा
(नवगठित कटिहार जिला) अक्सर पानी में डूबा रहता था। इन रिपोर्टों के अनुसार कटिहार
की इस दुर्गति में केवल महानन्दा का ही नहीं बल्कि कारी कोसी तथा गंगा नदी का भी
यथेष्ट योगदान रहा करता था।
महानन्दा
की सहायक धाराओं की यह खासियत रही है कि उनके भी न सिर्फ रास्ते बदलते रहे हैं
बल्कि उनके नाम भी उसी तरह बदलते रहते हैं। मसलन पनार नदी के कितने ही नाम हैं
जैसे पनार, परमान, परमौं, कदवा, रीगा, कंकर, फुलहर
या फिर गंगाजुरी। जैसे-जैसे जगहें बदलती हैं नदियों के नाम भी बदलते रहते हैं।
इसी तरह बकरा नदी का नाम अलगअलग स्थानों पर बकरा, कतुआ
धार या देवनी हो जाता है। कनकई की कितनी ही नई, पुरानी
धारायें उसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र पर बिखरी पड़ी हुई। हैं और लगभग ऐसी ही स्थिति
मेची, दाऊक, रमजान, कुलिक, सुधानी
और नागर नदियों की भी है। इन नदियों की धाराओं का विभाजन होता रहता है, उनसे
होकर गुजरने वाले जल प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है और उसी तरीके से
उनका महत्व भी घटता-बढ़ता रहता है। अंग्रेजों के शासन की स्थापना के बाद इस
क्षेत्र का एक सर्वेक्षण जेम्स रेनेल नाम के एक सैनिक इन्जीनियर ने सबसे पहले 1779 में
किया था। उस समय के महानन्दा के प्रवाह पथ का आधिकारिक विवरण रेनेल के नक्शे से
मिलता है। उसके बाद डॉ० फ्रान्सिस बुकानन हैमिल्टन (1809-10),
रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (1838),
तथा डॉ० डब्लू० डब्लू० हन्टर (1877) ने भी
नदी के प्रवाह पथ का विवरण दिया है।
महानन्दा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह आर्यों के प्रभाव का अन्तिम पूर्वी छोर है और इस क्षेत्र का इतिहास पश्चिम से आये आक्रान्ताओं तथा मूल निवासियों के बीच संघर्षों का रहा है।

इम्पीरियल
गजेटियर ऑफ इन्डिया के अनसार ‘महानन्दा
पश्चिम के हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा पूर्व के बांग्ला भाषी क्षेत्रों के बीच सीमा
का काम करती है और जनसंख्या के आँकड़े, जिसके
अनुसार हिन्दी भाषी जनसंख्या का प्रतिशत 94-6 है
जबकि केवल 5 प्रतिशत लोग बांग्ला भाषी
हैं, विश्वसनीय नहीं लगते ।
डा० ग्रियर्सन का अनुमान है कि लगभग एक तिहाई लोग बांग्ला बोलते होंगे और यह ठीक
लगता है। महानन्दा एक धार्मिक सीमा रेखा का भी काम करती है जिसके पूर्व में दो
तिहाई (पूर्णिया जिले में) बाशिन्दे मुसलमान होंगे जबकि पश्चिम में उनकी संख्या एक
तिहाई से कम होगी।
परन्तु कोसी की चर्चा किये बिना महानन्दा का जिक्र अधूरा रह जायेगा। कोसी नेपाल तथा बिहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो कि हिमालय पर्वत की मुख्य श्रृंखला में 5,400 मीटर की ऊँचाई से निकल कर तिब्बत, नेपाल तथा उत्तर बिहार के लगभग 725 कि० मी० रास्ते को तय कर के कुरसेला (कटिहार) के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार में इस नदी की लंबाई 254 कि० मी० है जबकि इस नदी की मैदानों में कुल लंबाई 307 कि० मी० है। सुन कोसी, तामा कोसी तथा अरुण कोसी नाम की तीन धाराओं के संगम से बनी कोसी नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 58,594 वर्ग कि० मी० है जिसमें से 5,704 वर्ग कि० मी० ग्लेशियर है।

पौराणिक
लेखों, किंवदन्तियों, लोक
कथाओं तथा लोक गीतों के अलावा कोसी के बारे में लिखित जानकारी अंग्रेजों के द्वारा
ही तैयार की गई। उनके यात्रा वृत्त तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों आदि में इस नदी की
काफी चर्चायें हुयी हैं यद्यपि उनका मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों की प्राकृतिक
सम्पदाओं का दोहन और राजस्व की वसूली था। फ्रान्सिस बुकानन (1809-1810)
तथा रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (1838) के
यात्रा वृत्त तथा हन्टर द्वारा लिखित पुस्तक श्रृंखला “स्टैटिस्टिकल
अकाउन्ट्स ऑफ बंगाल' (1877) में इस
नदी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इन रिकार्डों से पता लगता है कि कोसी अपने
अत्यधिक सिल्ट के कारण धारा परिवर्तन के लिये लम्बे समय से बदनाम रही है। 1736 से 1955 के बीच
के उपलब्ध रिकार्डो से अन्दाजा लगता है कि इस दौरान यह नदी जो कि कभी पूर्णियाँ के
पूर्व होकर बहती थी अब खिसकते-खिसकते 110 कि०
मी० पश्चिम की ओर हटी है तथा सुपौल, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया
जिलों से होती हुई गंगा से जा मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोसी कभी
मालदा (पश्चिम बंगाल) होकर बहती थी और बुकानन हैमिल्टन के अनुसार तो यह नदी मालदा
के पूर्व में भी बही होगी। बुकानन लिखते हैं, “कोसी
के किनारों पर रहने वाले स्थानीय विद्वान या पण्डित तो यहाँ तक कहते हैं कि
प्राचीन काल में कोसी दक्षिण पूर्व दिशा में ताजपुर तक बहती थी। जिसके बाद इसका
प्रवाह पूर्व की ओर हो जाता था और यह अन्ततः ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती थी और
गंगा से इसका कोई वास्ता ही नहीं था। इस कथन का आधार क्या है यह तो मैं नहीं जानता, कि यह
लोक कथ्य है या किंवदन्ति। अगर यह किंवदन्ति है तो यह बात थोड़ी अधिक विश्वसनीय हो
जाती है। परन्तु ऐसा होना काफी कुछ संभव सा लगता है। हो सकता है कि मालदा के पूर्व
और उत्तर में स्थित बड़ी-बड़ी झीलें कभी कोसी और महानन्दा के अवशेष हों।
...उपर्युक्त परिवर्तनों में कोसी में कम-से-कम कम्पनी की सीमा में कोई नदी बायें
तट पर संगम नहीं करती है परन्तु इससे बहुत सी धारायें फूटती हैं। उत्तर के पहाड़ों
से आने वाली बहुत-सी नदियाँ अब महानन्दा में आकर मिलती हैं और यह बहुत संभव है कि
यह नदियाँ पहले कोसी में मिलती रही हों जबकि इसकी धारा उत्तर पूर्व की ओर रही हो
...।
हन्टर
(1877) लेकिन बुकानन के इस विचार
से सहमत नहीं थे, उनका
कहना था कि, “डा० बुकानन हैमिल्टन का
यह कहना कि कोसी ब्रह्मपुत्र से मिलती रही होगी उनके बाकी के सिद्धांतों के
मुकाबले जरा कम मुमकिन लगता है। ऐसा लगता है कि पूर्व काल में ब्रह्मपुत्र का
प्रवाह पथ मैमनसिंह के भी पूर्व में था। कोसी अपने पूर्व की ओर के प्रयाण में
पहले करतुआ से मिलेगी जो कि खुद एक अच्छी खासी नदी है और जिसमें आत्रेयी तथ तीस्ता
का पानी आता था। मैंने अपनी पुस्तक अकाउन्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोगरा (खण्ड VIII पृ० 139,
142, 162) में आदि हिन्दू काल से आकार तथा महत्व के आधार पर इस नदी की
महत्ता को रेखांकित किया है और यह कहा था कि यह नदी स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में
मानव प्रजाति की एक सीमा रेखा का काम करती है जो कि आज तक दिखाई पड़ता है। अगर हम
यह मान सके कि कोसी तथा महानन्दा पहले करतुआ में जाकर मिलती थीं तो हमें पूर्व काल
में करतुआ के बड़े आकार का कारण समझ में आ जायगा और तब राजशाही जिले के बारिन्द्र
तथा मैमनसिंह जिले के मधुपुर के जंगलों के बीच दिखाई पड़नेवाले बालू के मैदानी
इलाकों का औचित्य भी स्पष्ट हो जायगा जिनसे होकर इस शताब्दी के प्रारंभ में
ब्रह्मपुत्र बहा करता था।
वास्तव में पूर्णियाँ से लेकर दरभंगा तक के बीच
एक इंच भी जमीन ऐसी
नहीं है जिस पर कभी कोसी की धारा न बही हो। इसकी विभिन्न धाराओं के कितने ही नाम हैं--सौरा, बरण्डी, कारीकोसी, मराकोसी, तिलावे
धार, हइयाधार, बोचहा
धार, मझारी धार, धेमुरा
धार, मिरचाइया धार, लगुनिया
धार आदि-आदि। जिस धारा से होकर कोसी की मुख्य धारा बही वही कोसी हो गई। इस तरह
कोसी और महानन्दा के बीच का क्षेत्र हमेशा बाढ़ और जल जमाव का क्षेत्र रहा है
जिसका अधिकांश श्रेय कोसी को जाता है।
मगर
जहाँ तक बाढ़ का प्रश्न है कोसी के नक्कारखाने में महानन्दा की तूती सिर्फ कभी-कभी
सुनाई पड़ी है।
घने
जंगलों, दुर्गम रास्तों और
थोड़े-थोड़े फासले पर नदियों का मौजूद रहना--संम्भवतः
इन्हीं सब कारणों से पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास के लिये इस इलाके को चुना होगा जो कि पौराणिक कथाओं में
बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र महाभारत काल में कर्ण
के अधीन था। कुरसेला, जहाँ
कि कोसी गंगा में मिल जाती है, कौरवों
के राज्य में पड़ता था और इसका नाम तब कुरुशिला था। कभी मनिहारी (कटिहार) का मूल
नाम मणिहरण था जहाँ भगवान श्री कृष्ण के अंगूठी की मणि खो गई थी।
सिमल
वन जहाँ अर्जुन ने अज्ञात वास के पहले अपने अस्त्र-शस्त्र छिपाये थे, वर्तमान
सेमापुर है जो कटिहार-बरौनी मार्ग पर एक रेलवे स्टेशन है। इसी तरह किशनगंज जिले के
ठाकुर गंज कस्बे के बारे में यह किंवदन्ती है कि यह राजा विराट के राज्य का हिस्सा
था और यहीं भीम ने रसोइया (ठाकुर) बनकर अपना अज्ञातवास काटा था। इस कस्बे में
भातढाला और सागढाला नाम के दो तालाब हैं जिनमें कभी भीम भात और साग रखा करते थे।
ठाकुर गंज से कुछ फासले पर ही वह स्थान है जहाँ भीम ने कीचक का वध किया था।
इस
जिले से बाहर आने वालों के मुकाबले बाहर जाने की परम्परा उल्लेखनीय है। पूर्णिया
के लोग खेतों में कड़ी मेहनत से परहेज करते हैं और रोजी रोटी की तलाश में जिले से
बाहर जाना भी ये पसमद नहीं करते। क्षेत्रफल को देखते हुए आबादी कम है, जमीन
आसानी से उपलब्ध है और लगन कम है। यह कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से पूर्णियाँ के
लोगों को बाहर जाने से अरुचि है। एक अच्छी खासी तादाद में खेती के मौसम में
अस्थायी रूप से बहुत बड़ी जनसंख्या पूर्णियाँ आती है। यह बात 1963 में
कही गई। आज हालत यह है कि वर्षा समाप्त होने के तुरन्त बाद अपने यहाँ धान, भदई और
जूट की कटाई की परवाह किये बगैर इस इलाके का मजदूर रेल गाड़ियों की छतों पर सवार
होकर पंजाब, हरियाणा, असम, कलकत्ता
या फिर गुजरात और महाराष्ट्र का रुख करता है। रेल गाड़ियों की छत पर बैठने पर
अक्सर दुर्घटनायें हो जाती हैं जिसमें लोग मरते हैं और कोसी, महानन्दा
दोआब के लोग ऐसी घटनाओं में मरे हैं। वे इमारतें ढहने पर भी मरे हैं और खाड़कुओं
के हाथों भी मरे हैं। 1963 से 1993 के बीच
कुछ ऐसा जरूर हो गया कि पूर्णियाँ के खेतों में कड़ी मेहनत से परहेज करने वाले तथा
रोजी रोटी की तलाश में जिले से बाहर जाना न पसन्द करने वाले लोग अपनी जान की कीमत
पर भी। दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने और बाहर जाने के लिये मजबूर हो गये।
जबकि कभी हालत यह थी कि “फसलों
की कटाई के समय, और जब असम के चाय बगानों
में मजदूरों की जरूरत पड़ती है तब, कटिहार
और उससे आगे जाने वाली रेलगाड़ियों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के विभिन्न हिस्सों
से आये मजदूरों की बेशुमार भीड़ रहा करती थी। वास्तव में फसलों की कटाई के समय
यदि ऐसे मजदूर पूर्णियाँ न जाये तो फसलों, खासकर
जूट, की कटाई तो हो ही नहीं
पायेगी। खुशहाली से बदहाली तक का यह सफर पिछले तीस साल में तय किया गया।
पिछले
चार दशकों में हुये विकास का प्रभाव इस तरह साफ तौर पर उलटा दिखाई पड़ता है।
कोसी-महानन्दा के दोआब का यह इलाका मजदूरों के लिहाज से एकाएक सरप्लस कैसे हो गया।
इसका एक कारण इस इलाके में साल दर साल आने वाली बाढ़ है जिससे अधिकांश जमीन पर
काफी समय तक पानी लगा रहता है और खेती संभव नहीं हो पाती। यद्यपि हम बाढ़ को इस
परिस्थिति का अकेला कारण नहीं मानते क्योंकि आज अगर उत्तर बिहार में बाढ़ है तो
दक्षिण बिहार में सूखा है परन्तु विकास का परिणाम वहाँ भी लोग करीब वैसा ही भुगतते
रहे हैं जैसा कि उत्तर बिहार के लोग।
वहाँ
तो बाढ़ नहीं है फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, वहाँ
भी लोग मजदूरी की तलाश में बाहर जाते हैं।''14 परन्तु
साथ ही हमारे लिये यह पचा पाना भी मुश्किल है यह सारा कुछ जनसंख्या की वृद्धि के
कारण है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की सबसे अधिक संभावनायें हैं। अतः
किसी तरीके से खेती बची रह जाय तो बहुत से लोग जमीन से जुड़े रह जायेंगे और
रेलगाड़ियों की छतों पर भीड़ कुछ कम हो जायगी।
महानन्दा तो नहीं, पर कोसी की बाढ़ पर चर्चा पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से चल रहा है। परे भारत में बाढ़ लाने वाली नदियों के बीच कोसी की मिसाल दी जाती है और यह नदी किसी भी बाढ़ चर्चा के केन्द्र बिन्दु में रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस नदी को नियंत्रित करने के प्रयास किये गये और इसी के साथ लगभग पूरी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र घाटी की नदियों को काबू में करने के लिये हाँको शुरू हुआ और इसी क्रम में महानन्दा का भी नम्बर आ गया।
(प्रख्यात नदी विशेषज्ञ एवं पर्यावरणविद डॉ. दिनेश कुमार मिश्र जी की पुस्तक "बंदिनी महानंदा" से उद्घृत)